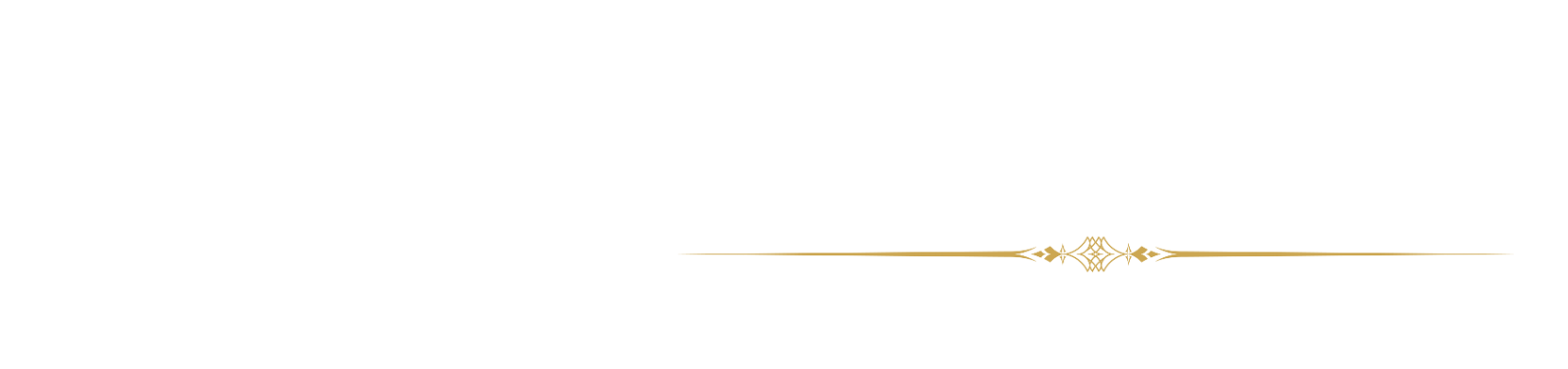झूठी कहानी

अस्र का वक़्त है या शायद उस के कुछ बाद का। मग़रिब तक मुझे घर पहुँच जाना चाहिये। “पहुँच जाउंगी” इर्द-गिर्द देखते हुए मैं एतिमाद से ख़ुद को बताती हूँ और अपने क़दम तेज़ कर देती हूँ। मेरे ज़ह्न में कुछ देर पहले के वाक़आत घूमने लगते हैं। मैं उन्हें ख़ूब अच्छी तरह दोहराने और याद करने की कोशिश करती हूँ ताकि घर जा कर सब को बता सकूँ कि क्या हुआ था। सब को इंतिज़ार होगा। सब पूछेंगे, बताओ क्या हुआ था?
मैं फिर अपनी याद्दाश्त मुरत्तब करने लगती हूँ। वाक़आत मुझे अच्छी तरह याद हैं लेकिन बार-बार सोचने से वो कुछ धुंधलाने लगते हैं। जैसे गिलास पर गीले हाथों के निशान थोड़ी देर में ही कहीं-कहीं से मिटने लगते हैं। जहाँ-जहाँ गीलाहट महसूस होती है वहाँ-वहाँ मैं नज़रें जमा देती हूँ और उन मिटते हुए निशानों की मदद से मिट गए हुए निशानों को समझने की कोशिश करती हूँ।
ऐसा क्यूँ होता है? आधी बातें याद रहती हैं और आधी बातें भूल जाती हैं? जो भूल जाती हैं वो भी पूरी तरह नहीं भूलतीं बल्कि उन के धब्बे याद्दाश्त की स्लेट पर मुसलसल मौजूद रहते हैं। कभी-कभी इन धब्बों से शक्लें सी बन जाती हैं। कभी-कभी वो शक्लें पहचानी भी जाती हैं लेकिन उमूमन ऐसा नहीं होता। बस इंसान सारी उम्र यही सोचता रहता है, ये क्या था? कैसे था? क्यूँ था? कुछ याद नहीं आता, सिवाय इस के कि कुछ था ज़रूर।
मैं अपने ख़यालों में गुम तेज़ी से चलती हूँ कि अचानक मेरा रास्ता मुझे रोक लेता है। रुक कर अपनी तरफ़ देखने पर मजबूर करता है। जो बे-ध्यानी से, मगर इस यक़ीन के आलम में चली जा रही थी कि घर जा रही हूँ, वो ध्यान टूट सा जाता है।
मैं चौंक कर इधर-उधर देखती हूँ। दोनों तरफ़ के मंज़र ना-मानूस मालूम होते हैं। अजनबीयत फ़र्श से उठ-उठ कर मेरे गले पड़ती मालूम होती है। जैसे आँधी चले तो धूल आँखों में घुस कर आप जता देती है।
ये कौन सी गली है? बाग़बान-पुरे की? नहीं, अनारकली की?
नहीं, अनारकली तो नहीं, कोई और, नहीं?
पहचानी क्यूँ नहीं जा रही?
मैं तो हज़ारों दफ़ा यहाँ से गुज़री हूँ। हर बार घर जाने के लिये यहीं से तो गुज़रती थी। ओल्ड कैम्पस से निकल कर घर जाने के लिये।
ओल्ड कैम्पस?
मेरा ज़ह्न किसी और ही ज़मान-ओ-मकान में भटकने लगता है। फिर अचानक याद आता है कि मैं ओल्ड कैम्पस में नहीं पढ़ती थी, मैं तो न्यू कैम्पस में थी। और घर कैसा? तब तो मैं हॉस्टल में रहती थी।
“हाँ ठीक है। हॉस्टल में थी लेकिन अनारकली तो अकसर आना होता था। अनारकली से घर जाते हुए…”
मेरा ज़ह्न फिर भटक जाता।
मुझे अपनी उलझन पर उलझन होने लगती है और मैं झल्ला कर अपनी सोच को झटक देती हूँ।
“अच्छा चलो, जो भी है, मैं इन रास्तों से तो कई बार गुज़री हूँ। मैं ज़रूर घर पहुँच जाउंगी।”
मैं ख़ुद को तसल्ली देती हूँ। लेकिन दिल में ख़दशा सा होने लगा है इस लिये मैं गली को ख़ूब अच्छी तरह, ग़ौर से देखने और पहचानने की कोशिश करती हूँ।
कभी दाएँ और कभी बाएँ
मुझे महसूस होता है गली पहले की निस्बत तंग होती जा रही है और दोनों तरफ़ की दुकानें ऊपर चढ़ती हुई महसूस हो रही हैं। मैं घबरा कर नीचे देखने लगती हूँ, फ़र्श पर पत्थर भी उखड़-उखड़ कर बाहर निकल रहे हैं। ऊँचे-नीचे, ग़ैर-हमवार, गंदगी से लिथड़े हुए काले पत्थर, जिन से किसी को भी ठोकर लग सकती है।
“ग़रीब लोग यहाँ कैसे गुज़ारा करते हैं?”
एक उचटता हुआ ख़याल मेरे ज़ह्न से टकरा कर गुज़रता है और मुझे ख़ुद पर शर्म आती है।
“मुझे आज बरसों बाद इस गली से गुज़रना पड़ा है तो मैं कैसी झल्ला रही हूँ। ये ग़रीब लोग, जो यहीं रहते हैं, यहीं जीते-मरते हैं, उन के बच्चे इन्ही फ़र्शों पर खेल-खेल कर बड़े हो जाते हैं, उन के जनाज़े इन्ही गलियों से निकलते हैं।”
साथ ही मुझे एहसास होता है कि मैंने कितनी आसानी से ख़ुद को इन ग़रीब लोगों से जुदा कर लिया है।
“ग़रीब लोग” कह कर मेरे अंदर अपनी बड़ाई का, उन से अलग होने का, जो तमानियत भरा एहसास पैदा हुआ है उस का तअफ़्फ़ुन मेरे वुजूद का हिस्सा बन गया है।
“मैं ख़ुद भी कभी इन्हीं गलियों का रोड़ा थी।”
मैं इस तअफ़्फ़ुन को झाड़ने की निदामत भरी मगर नाकाम कोशिश करती हूँ।
मेरा दिल भर आता है और मैं गली के दोनों सम्तों में बे-तरतीबी से बनी छोटी-बड़ी दुकानों को देखने लगती हूँ। सब के अंदरूनी मंज़र एक से तारीक हैं। बिजली के, मक्खियों के फ़ुज़्ले से अटे हुए तारों से लटके हुए चालीस वॉट के बल्ब जिन की पीली-पीली रौशनी ढलते दिन के उदास दिन के साथ मिल के एक मायूस-कुन माहौल पैदा कर रही है। किसी जाली आमिल या जादूगर की कोठरी जैसा, जिस में हड्डियों के जलने की आवाज़ और गोश्त के जलने की बू होती है।
मैं देखती हूँ, एक दुकान पर बान की रस्सियाँ पड़ी हैं। कुछ लोगों की शक्ल में लिपटी हुई, कुछ बड़े-बड़े लच्छों की सूरत में। दुकानदार एक मोटी तोंद वाला आदमी है, जिस ने मटमैला सा सफ़ेद कुर्ता पहन रखा है और वो एक हाथ में बान की रस्सी का लच्छा पकड़े हुए है, और दूसरे हाथ में गोला। पता नहीं वो गोले का लच्छा बना रहा है या लच्छे का गोला। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता लेकिन उस की शक्ल देख कर कोई ना-गवार सा एहसास मुझे अपने अंदर बाओ गोले की सूरत उठता महसूस होता है। मैं मुँह मोड़ कर दूसरी तरफ़ देखने लगती हूँ।
एक तेली की दुकान नज़र आती है। काले-काले पीपों में काला-काला तेल। वो एक पीपे को उलट कर उस का तेल शीशे की एक तंग बोतल में डाल रहा है। बोतल के मुंह पर सिलवर की क़ीफ़ पड़ी है जो कभी सफ़ेद होती होगी लेकिन अब बिल्कुल काली हो चुकी है। मैं इस मंज़र में मह्व हो जाती हूँ, पूरे ध्यान के साथ। मुझे डर लगता है कि अभी सारा पीपा उलट जाएगा और तेल ज़मीन पर बह जाएगा। मैं एहतियातन अपनी साँस रोक लेती हूँ और काफ़ी देर तक रोके रखती हूँ। फिर अचानक मेरा दम घुटने लगता है तो मुझे एहसास होता है, तेल का पीपा मैं नहीं तेली उलट रहा है। मेरे साँस रोक लेने से तेल का बह जाना रुक नहीं सकता। मैं ये मशक़्क़त-नुमा एहतियात बिला-वजह कर रही थी। मुझे ख़ुद पर ग़ुस्सा आने लगता है। मैं यूँ ही अपने साथ ज़ुल्म करने की आदी हूँ। दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़ुद पर बिता-बिता कर मैंने ख़ुद को वक़्त से बहुत पहले बूढ़ा कर लिया है। इस लिये मैं ज़िंदगी के लुत्फ़ से महरूम हो गई हूँ। ज़िंदगी, जो एक ही दफ़ा मिलती है, इसे भरपूर तरीक़े से जीना तो चाहिये। मैं यूँ ही दूसरों की फ़िक्र कर-कर के अपने जीने का अमल बे-लुत्फ़ करती रहती हूँ।
मुझ पर एक बेज़ार-कुन मायूसी और बेदिली सी छा जाती है। गली कुछ और तंग होती महसूस होती है। मैं अपने क़दम और तेज़ कर देती हूँ कि अभी इधर से मुड़ कर एक दो गलियाँ और होंगी फिर घर आ जाएगा। ये गली बस ख़त्म होने को है।
सामने एक घर या दुकान का काम जारी है। लोग कुछ ज़्यादा हो गए हैं। मुझे अपने जिस्म पर नज़रों के पत्थर बरसते हुए महसूस होते हैं। मैं सर उठा कर देखती हूँ। बहुत से लोग खड़े शोर मचा रहे हैं। शायद लेंटर डाला जा रहा है। सिमेंट की भरी हुई तग़ारियाँ उठा-उठा कर ऊपर पहुँचाई जा रही हैं। साथ-साथ ऊँची आवाज़ में क़हक़हे लग रहे हैं। उन के हाथों में सिमेंट की तग़ारियाँ हैं, उन के इर्द-गिर्द गीली ईंटों के ढेर हैं। एक तरफ़ गली में सरिया पड़ा है। लम्बे-लम्बे नेज़े गली में बिछ गए हैं और वो ज़ोर-ज़ोर से हंस रहे हैं।
किस पर हंस रहे हैं?
मुझ पर?
मैं जो अकेली यहाँ से गुज़र रही हूँ।
मैं जो एक औरत हूँ।
एक औरत जो अकेली इस वक़्त गली से गुज़र रही है।
हा हा हा!
ये औरत ज़रूर कोई…
शायद वो एक-दूसरे को आँख मारते हैं और क़हक़हे लगाते हैं। मेरी ख़ुद-एतिमादी ख़त्म हो जाती है। मैं अंदर से लरज़ने लगती हूँ और क़दम तेज़ कर देती हूँ लेकिन गली फ़ौरन ख़त्म हो जाती है और ख़त्म होने से ज़रा पहले एक और गली का सिरा उस में खुलता दिखाई देता है। मैं तेज़ी और क़दरे बदहवासी से उस गली में दाख़िल हो जाती हूँ।
ये दूसरी गली टेढ़ी-मेढ़ी और छोटी सी है। बिल्कुल सामने कुब निकालती हुई दाएँ हाथ को मुड़ती है लेकिन मुझे बिल्कुल अजनबी महसूस होती है। उस गली से मानूसियत की कोई लहर नहीं उठती। कुछ भी जाना पहचाना नहीं। नीम जाना-पहचाना भी नहीं। एक दम अजनबी।
तो क्या मैं रास्ता भूल गई हूँ?
ये ख़याल पहली बार मेरे शुऊर से टकराता है और मुझे लगता है ये ख़याल पहले भी मेरे ज़हन में मौजूद था लेकिन मैं इसे अपने शुऊर में आने से रोक रही थी। मैं जानती थी मैं रास्ता भूल रही हूँ लेकिन मैं ख़ुद को ये फ़रेब देना चाहती थी कि मुझे रास्ता मालूम है।
टेढ़ी-मेढ़ी गली में कोई चीज़ भी जानी-पहचानी नहीं लग रही। मैं एक लम्हे के लिये रुक कर इधर-उधर देखती हूँ। अब क्या करूँ? वापस जाऊँ या इसी गली में आगे बढ़ जाऊँ? कहीं न कहीं से तो रास्ता मिल ही जाएगा।
लेकिन अगर दाएँ मुड़ने वाली गली बंद हुई तो?
मुझे याद आता है इन इलाक़ों में गलियाँ कितनी पुरपेंच और गुमराह-कुन होती हैं। मग़रिब की तरफ़ मुड़ो तो मशरिक़ की तरफ़ ले जाती हैं। कहीं मैं किसी और ही सम्त न निकल जाऊँ?
किस सम्त में? दुनिया में बस चार ही सम्तें हैं क्या? कोई और सम्त होती तो किस तरफ़ होती?
एक फ़लसफ़ियाना सा सवाल शरीर ज़िद्दी बच्चे की तरह मेरे ज़ह्न से सर निकालता है और मैं बद-मिज़ाज माँ की तरह उसे चपत मार कर वापस धकेल देती हूँ।
मैं रास्ता भूल गई हूँ और इधर ये ज़ह्न कम-बख़्त सम्तों की तादाद और अब’आद पर ग़ौर करने चला है। मुझे अपने ज़ह्न पर ग़ुस्सा आने लगता है जो हमेशा बे-वक़्त चौकस हो जाता है और जब ज़रूरत होती है तो काम नहीं आता।
अब बताओ भला, मुझे याद ही नहीं आ रहा किस तरफ़ जाना था। अब क्या करूँ, इसी गली में चलती जाऊँ या वापस हो जाऊँ? हो सकता है मैं पहले ही ग़लत गली में दाख़िल हो गई हूँ।
मुझे वापस जा कर दूसरी गली में दाख़िल होना हो, जो घर तक जाती हो।
ये कश्मकश के चंद लम्हे मुझ पर क़यामत की तरह भारी होते हैं। फ़ैसला करना मुझे हमेशा मुश्किल लगता है। मेरी ज़िंदगी की नाकामियों की सब से बड़ी वजह ये है कि मैं दो इम्कानात में से एक को चुनने का फ़ैसला जल्दी और क़तईय्यत से नहीं कर सकती। चुनती एक को हूँ और देखती दूसरे को रहती हूँ। ख़ैर, ये तो मेरी शख़्सी कमज़ोरी है, अल्लाह मुझे मुआफ़ करे, कर ही देगा। उसी ने मुझे ऐसा बनाया है, लेकिन अब कहाँ जाऊँ?
मेरा ख़याल है मुझे किसी से पूछ लेना चाहिये।
मगर किस से पूछूँ?
जो ज़रा शरीफ़ दिखाई देता हो, जो मुझे ग़लत न बताए, जो मेरी तरफ़ गंदी नज़रों से न देखे। “आओ मेरे साथ आ जाओ।” कहती ग़लीज़ और मकरूह नज़रें, जो मेरे जिस्म पर ऐसे गिरती हैं जैसे किसी ने पेशाब की धार मार दी हो – गर्म-गर्म, बदबूदार, पीले पेशाब की धार।
मेरे अंदर मितली होने लगती है और मैं लड़खड़ाने लगती हूँ।
किस से रास्ता पूछूँ?
मुझे याद आता है गली मुड़ने से पहले बाएँ हाथ एक चाय वाला नज़र आया था। सर पर गोल टोपी और गले में मटियाला सा कुर्ता। वो सिल्वर के पव्वे को को हाथ में पकड़े चाय उछाल रहा था और बड़ी तवज्जो से अपना काम कर रहा था। यहाँ तक कि मेरा गुज़रना भी उस की नज़र से नहीं गुज़रा।
चाय वाले से पूछती हूँ, इसे ज़रूर मालूम होगा।
मुझे मालूम नहीं मैंने चाय वाले को क्यूँ मुंतख़िब किया। उस की गोल टोपी की वजह से। उस की अपने काम मे महवियत की वजह से या उस की बे-नियाज़ी की वजह से।
वापस मुड़ कर मैं दोबारा उसी पिछली गली में दाख़िल होती हूँ।
चाय वाले के पास रुक कर उस से पूछती हूँ ये गली मुड़ कर कहाँ निकलती है? लेकिन चाय वाले के जवाब देने से पहले ही मेरे इर्द-गिर्द एक हुजूम जमा हो जाता है। नौजवान शरीर लड़कों का हुजूम। वो सब दाँत निकाल रहे हैं। मुझे रास्ता बता रहे हैं लेकिन हर एक अलग-अलग रास्ता बताता है। उन के लहजे बताते हैं कि उन्हें ख़ुद कुछ मालूम नहीं। वो महज़ अपनी ला-इल्मी छुपा रहे हैं। लेकिन उन में से हर एक के अंदाज़ में इतना तयक़्क़ुन है जैसे मैंने उस की बात न मानी तो वो मुझे ज़बरदस्ती उस तरफ़ ले जाएगा।
सामने ही मज़दूरों का पूरा जत्था जमा है। उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है और तग़ारियाँ ज़मीन पर रख कर सब टकटकी बांध कर मेरी तरफ़ देख रहे हैं।
अब मैं वाक़ई घबरा जाती हूँ। मैं अपने लहजे को दुरुश्त और ख़ुद-एतिमाद बनाते हुए डाँट-डाँट कर लड़कों को पीछे हटने को कहती हूँ। मगर वो सब पूरी तरह लुत्फ़ उठाने के मूड में हैं।
एक नौजवान लड़की…
मगर मैं तो अब नौजवान नहीं रही। ये उम्र गुज़रे तो मुद्दतें हो गईं।
अच्छा तो एक फ़ैशनेबल औरत…
लेकिन मैं कहाँ फ़ैशनेबल हूँ। मैं तो…
हा हा हा… कटे हुए बालों वाली बूढ़ी औरत… जो इन के नरग़े में है और इन से रास्ता पूछ रही है। वो अपनी ज़िन्दगी के इस अनोखे मौक़े से पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन पर कोई असर नहीं होता। मैं चिल्लाने लगती हूँ जिस पर वो और हंसते हैं।
मैं बेबसी से चाय वाले की तरफ़ देखती हूँ। वो उसी बे-नियाज़ी से पव्वे से चाय उंडेल रहा है।
फिर मेरे चिल्लाने पर वो एक तरफ़ हट जाते हैं और मेरा रास्ता खुला छोड़ देते हैं, जैसे कह रहे हों, अच्छा तो फिर जाओ जहाँ जाती हो। देखते हैं हम भी, रास्ता कैसे मिलता है।
ये बात वो मुँह से नहीं कहते मगर उन के पूरे वुजूद चिल्ला रहे हैं।
उन के बाहर निकले हुए दाँत, उन के चढ़े हुए अबरू, उन के कुर्तों की उलटी हुई आस्तीनें, उन के चेहरों पर हज़ उठाने की ख़्वाहिश।
मैं जल्दी से वापस उसी गली में मुड़ जाती हूँ और एक लम्बा साँस ले कर नए सिरे से याद करने की कोशिश करती हूँ।
क्या मैं पहले कभी इस गली से गुज़री हूँ?
अगर मैं यहाँ से सीधे निकल जाऊँ तो किसी तरफ़ को मुड़ कर घर तक पहुँच जाउंगी?
लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता।
ओफ़्फ़ो! मैं टैक्सी क्यूँ न ले लूँ? ओह मेरे ख़ुदा, ये ख़याल मेरे ज़ह्न में पहले क्यूँ नहीं आया? मैं एक लम्बी साँस ले कर अपनी बदहवासी को दुरुस्त करती हूँ।
हाँ ठीक है, मैं टैक्सी ले लेती हूँ।
मैं इधर-उधर देखती हूँ, कहीं कोई टैक्सी नज़र नहीं आती।
इन गलियों में टैक्सी कहाँ से आएगी। टैक्सी तो यहाँ से गुज़र ही नहीं सकती।
अच्छा तो फिर रिक्शा?
हाँ रिक्शा तो यहाँ से गुज़रता है। अभी थोड़ी देर पहले एक रिक्शा यहाँ से गुज़रा था और उसे जगह देने के लिये मुझे एक दुकान की दीवार के साथ जुड़ कर खड़ा होना पड़ा था।
अच्छा तो मैं रिक्शा ले लेती हूँ।
अब मुझे कुछ इत्मीनान होता है और मैं दाएँ कंधे से लटके अपने बैग को खोल कर देखती हूँ।
मेरा बटवा?
मैं घबरा कर दोबारा बैग में झाँकती हूँ।
बटवा कहाँ गया? पैसे तो उसी में थे।
मुझे याद आता है वो तो मैंने हाथ में पकड़ रखा था। हाँ, वो तो हाथ में पकड़ रखा था। हाँ वो हाथ में ही था जब मैं उन शरीर लड़कों से बात कर रही थी।
मैं जल्दी से अपने हाथ खोल कर देखती हूँ। घबराहट में अपने कपड़े झाड़ती हूँ। दोनों हाथ ख़ाली हैं। कपड़ों से भी कोई बरामदगी नहीं होती।
अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं घर जा कर रिक्शे वाले का किराया अदा कर दूंगी। मैं ख़ुद को इत्मीनान दिलाती हूँ और इस बात पर ख़ुद को शाबाशी देती हूँ कि मेरा ज़ह्न हर मुश्किल में कोई न कोई हल ढूंढ ही निकालता है।
अच्छा तो अब कोई ख़ाली रिक्शा ढूंढते हैं ताकि मग़रिब की अज़ान से पहले घर पहुँच जाऊँ।
रोज़ा खुलने से पहले।
मुझे याद आता है आज तो मेरा रोज़ा है।
लेकिन इस याद के साथ ही एक और ख़याल अचानक जस्त लगा कर अक़ब से उछलता है और सामने आ कर खड़ा हो जाता है। अभी इस गली में दाख़िल होने से पहले मैं जहाँ बैठी थी वहाँ तो मैंने पेट भर कर खाया पिया था।
चाय, पकौड़े, पेटीज़, और भी बहुत कुछ था। मैं सोफ़े पर पाँव रख के बैठ गई थी और जी भर कर खाती-पीती रही थी।
तो मेरा रोज़ा टूट चुका।
मेरा रोज़ा ज़ाया हो गया।
जैसे बच्चा ज़ाया हो जाए।
रोज़े के टूट जाने का अलम मेरे अंदर ऐसे उतरता है जैसे शीशे की बोतल में गाढ़े-गाढ़े तेल की धार। दीवारों के साथ-साथ चिपकी हुई, पूरी तरह लिथड़ जाती हुई।
अचानक गली में मग़रिब की अज़ान गूँजने लगती है।
रोज़ा खुल गया है।
लेकिन मेरा रोज़ा तो टूट चुका है।
अब घर जाने की जल्दी क्या है।
٠٠٠
नजीबा आरिफ़ उर्दू की प्रोफ़ेसर हैं, पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से उनका तअल्लुक़ है. कहानियां और नस्री नज़्में लिखती हैं. उनकी ये कहानी ‘सवेरा‘ की चुनी हुई नई उर्दू कहानियों के विशेषांक से ली गई है.
नजीबा आरिफ़ की इस कहानी में एक औरत की ज़हनी कश्मकश को उजागर किया गया है. एक औरत जो याददाश्त के धुंधलाते हुए नक़्श अपने ज़हन में देख सकती है. इस कहानी में वो रास्ता भटक गयी है या फिर अपने रोज़ के रास्तों को पहचानने की हालत में नहीं है. इस उलझन में वो बहुत कुछ भूल रही है, बहुत कुछ याद कर रही है. अचानक उसके आस पास की सारी दुनिया एक झूठ में बदल गई है.