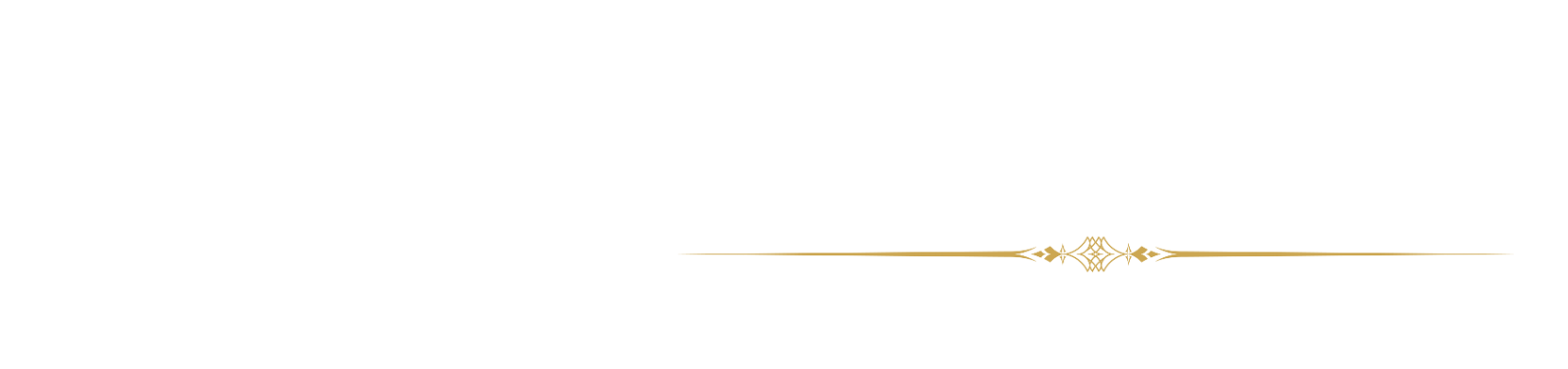दुंबाला-गर्द
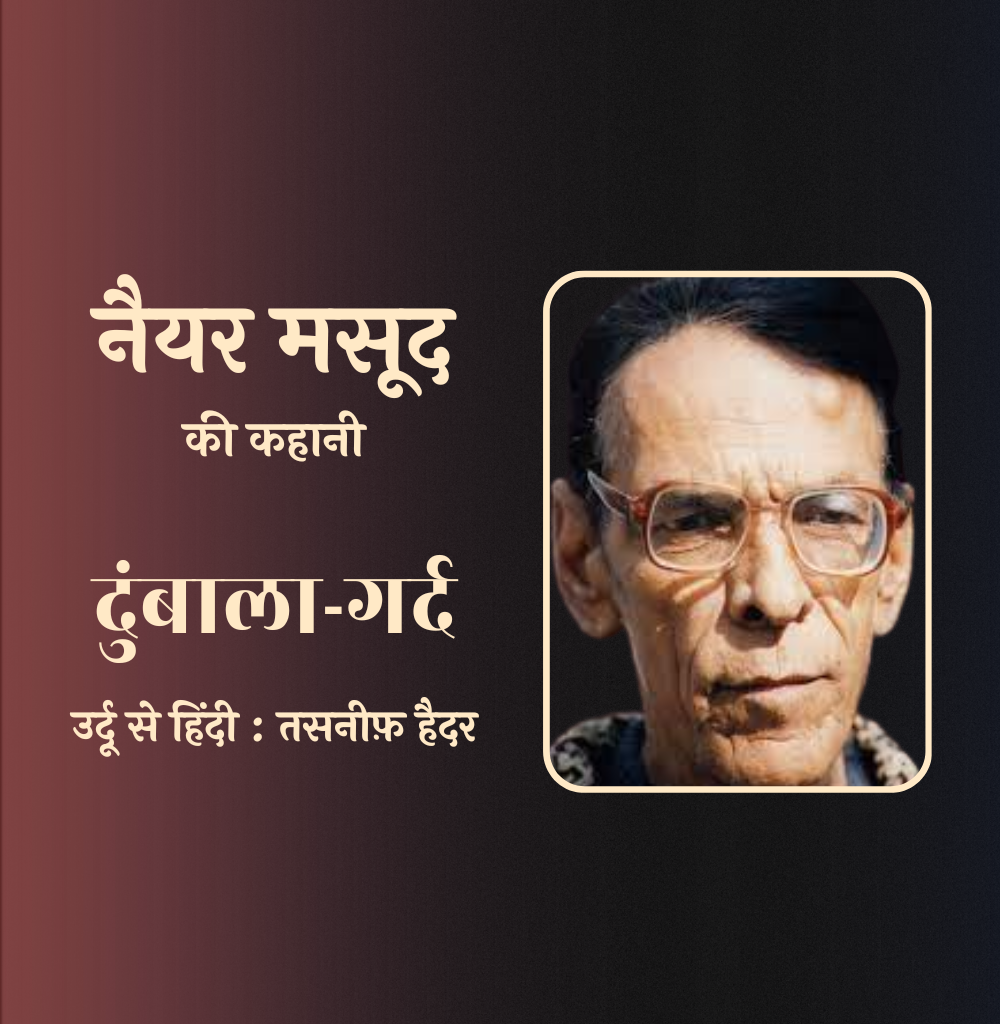
1
वह शहर से ज़रा हट कर घने दरख़्तों का एक झुंड था। उसके पीछे लम्बा सा मैदान था जिसकी ज़मीन हमवार कर दी गई थी. असल में यहाँ रेलवे लाइन बिछने वाली थी और उसके लिए ज़मीन बराबर की जा रही थी लेकिन बाद में वह लाइन किसी और तरफ़ बिछाई गई और यह मैदान यूँ ही पड़ा रह गया। मैदान सड़क पर से नज़र नहीं आता था। वहां से सिर्फ बे-तरतीब जंगली झाड़ियाँ दिखाई देती थीं। उनके बाद ज़रा बुलंद और ना-हमवार ज़मीन का टुकड़ा था जिसके पीछे दरख़्तों के झुंड का सिर्फ़ ऊपरी हिस्सा झाँकता था। सड़क से समझ में नहीं आता था कि दरख़्त क़रीब क़रीब लगे हुए हैं या दूर दूर, न ये समझ में आता था कि दरख़्तों का सिलसिला कहाँ तक गया है।
एक दिन, जब मैं उधर से गुज़र रहा था, मुझे तजस्सुस हुआ कि इस झुंड को देखूं। उस दिन झुंड में पहुँच कर मुझ को ये बे-रौनक़ मैदान नज़र आया। इधर कोई नहीं आता था। कम से कम मेरा ख़याल यही था, इसलिए मुझको ये जगह चहल-क़दमी के लिए पसंद आई थी। ख़ुद चहल-क़दमी मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन शक किया गया था कि मेरे दिल में कोई ख़राबी पैदा हो रही है जिसको रोकने के लिए मुझ को सवेरे सवेरे ज़रा तेज़ क़दमों से चलना बताया गया था। दिल की बीमारी से उस वक़्त मैं डरता था। मुझे अचानक मर जाने के तसव्वुर से वहशत होती थी और बचपन के एक बुज़ुर्ग का क़ौल बार बार याद आता था। उनको अचानक मरने के बहुत से क़िस्से मालूम थे, मसलन एक साहब बेटे की बरात लेकर रवाना हो रहे थे। बरातियों को उन्होंने जल्दी कर के गाड़ियों पर सवार कराया। आख़िर में ख़ुद सवार होने के लिए पैर उठाया और गिर कर मर गए। बरात गाड़ियों से उतर पड़ी और उन साहब के आख़री इंतिज़ाम शुरू हो गए। बुज़ुर्ग इस तरह के क़िस्से मज़े ले ले कर बयान करते थे लेकिन बयान करने के बाद बड़े ग़ुस्से के लहजे में ये ज़रूर कहते थे :
‘ऐ साहब! ये बे-वक़्त मरना कैसा?’
एक और साहब का क़िस्सा भी बहुत बयान करते थे :
‘उनकी बेटी का रिश्ता लेकर बाहर से मेहमान आ रहे थे। ये उनके इन्तिज़ार में फाटक पर खड़े खड़े अख़बार पढ़ रहे थे। घर के अंदर अज़ीज़ रिश्तेदार जमा थे। दावत का इंतिज़ाम हो रहा था। मेहमान आ पहुंचे। यह उनका इस्तक़बाल करने बढ़ रहे थे कि लड़खड़ाए, अख़बार हाथ से छूट गया। मेहमानों ने लपक कर उनको संभाला, मगर वह दूसरी दुनिया में पहुँच चुके थे। लीजिये जनाब, कैसा रिश्ता, कहाँ की दावत। मेहमान जो मिठाई लेकर आए थे, वो उनके सामान ही में बंधी रह गई। बेचारे उनके कफ़न दफ़न में शरीक हो कर वापस चले गए।’ और फिर वही :
‘ऐ साहब, ये बे-वक़्त मरना कैसा?’
और ऐसा मालूम होता था कि वह हर बे-वक़्त मौत का ज़िम्मेदार मरने वाले को ठहरा रहे हैं। उन बुज़ुर्ग की बातों को सुन कर बचपन ही से मुझे अचानक मरने का ख़याल बुरा मालूम होता था और इसमें तरह तरह की क़बाहतें नज़र आती थीं। इसलिए मैंने सवेरे चहल-क़दमी का मशविरा मान लिया था। शहर के अंदर की सैरगाहों में मजमा बहुत रहता था। मैंने किसी वीरान मक़ाम की तलाश शुरू कर दी। इस तलाश में भी अच्छा ख़ासा चल लेता था। इसी तलाश में मुझे झुंड के पीछे ये मैदान मिला था। जाते हुए जाड़ों की सख़्त सर्दी का ज़माना था। मैं गर्म कपड़ों में ख़ुद को लपेट कर सुबह सवेरे निकल जाता था और मैदान में कहीं तेज़ क़दमों से, कहीं आहिस्ता आहिस्ता चलता था। लेकिन सर्दियां ख़त्म होते होते मैंने देखा कि वहां भी बहुत से लोग आने लगे हैं। उन में बूढ़े ज़्यादा थे। कई लोग तो लग भग दौड़ कर चलते थे, कुछ धीरे धीरे और लड़खड़ाते हुए चलते थे। उनको दूसरे लोग सवारियों पर पहुंचाते थे और मैदान में उनको छोड़ कर ख़ुद आराम से बैठे रहते थे। फिर उनको सवार करा के वापस ले जाते थे। मुझे इस मजमे के साथ अपना होना गवारा नहीं था लेकिन इस मैदान के सिवा कोई और मुनासिब जगह मेरे इल्म में नहीं थी। नाचार मैंने रात के आख़री हिस्से में, जब भी अँधेरा फैला होता, वहां जाना शुरू किया। इसमें नींद ख़राब होती थी लेकिन मैदान मुझे ख़ाली मिल जाता था और दूसरे लोगों के आने से पहले ही मेरी वापसी का वक़्त आ जाता था।
मेरा ख़याल था कि मैं वहां तन्हा होता हूँ लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि दरख़्तों के झुंड में कोई और भी मौजूद है। ये मुझको अपना वह्म मालूम होता था लेकिन एक दिन मैंने उसे देख लिया। उस दिन मुझे वापसी में देर हो गई थी और सुबह की रौशनी फैलने लगी थी। वह एक दरख़्त के तने से टेक लगाए बैठा हुआ था और मेरी तरफ़ उसकी तवज्जोह नहीं थी। दूसरे लोगों के आने का वक़्त क़रीब था, इसलिए मैं उसको ग़ौर से देखे बग़ैर झुंड से निकल कर शाहराह पर आ गया। उसके बाद कई बार मैंने उसको देखा, झुंड के पूर्वी किनारे पर, उसी दरख़्त के नीचे और घुटनों पर थोड़ी टिकाए हुए। अँधेरे में वह एक ख़याली सूरत की तरह नज़र आता था और मैं महज़ अंदाज़े से समझ लेता था कि वह बैठा हुआ है। मैंने कभी उसे मैदान में टहलते हुए नहीं देखा। न उसने कभी मेरी तरफ़ तवज्जोह की।
एक दिन मैं झुंड में से होता हुआ वापस जा रहा था कि उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैं रुक गया। वह उठ कर खड़ा हो चुका था। मैं उसके क़रीब आ गया :
‘क्या बात है?’ मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश करते हुए पूछा।
‘यहाँ दर्द हो रहा है,’ उसने बड़ी मुश्किल से कहा।
उसने दर्द की जगह की तरफ़ इशारा भी किया होगा, लेकिन अँधेरे में मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। वो गिरा पड़ रहा था। मैंने दोनों हाथों से उसे संभाला और दरख़्त के तने से टिका कर बिठा दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, इसलिए चुप चाप उसके क़रीब खड़ा रहा। शायद देर तक मैं उसके पास खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह की रौशनी फैल गई और दूसरे लोगों का आना बढ़ गया। रौशनी में उसने मुझे देखा और धीरे से मेरा नाम लिया।
‘तुम?’ उसने कहा, ‘यह तुम हो?’
मैंने भी उसे ग़ौर से देखा। वह मेरे दफ़्तर का कोई पुराना साथी था। लेकिन किस दफ़्तर का? मैंने शुरू में कई दफ़्तरों में कुछ कुछ दिन आरज़ी तौर पर काम किया था और अब मुझे वो सब दफ़्तर याद भी नहीं थे, न उन दफ़्तरों के किसी साथी का नाम याद था। वह उन्हीं दफ़्तरों में से किसी में काम करता था। उसके काँधे से एक चौकोर थैला लटका रहता था। थैला अब भी उसके काँधे से लटका हुआ था, और इसी की वजह से वह मुझे याद आ गया था। वह मुझसे पहले से इस दफ़्तर में काम कर रहा था। उसने कई मर्तबा दफ़्तरी मामलात में मेरी मदद भी की थी। उसका नाम छोटा सा था। लेकिन अब न उसका नाम मुझे याद आ रहा था, न यह कि वह किस दफ़्तर में मेरे साथ था। उससे मेरे ज़्यादा मरासिम नहीं थे। मैं हर दफ़्तर में अपने हम-उम्रों के साथ उठता बैठता था, वह मुझसे बड़ा था और मुझको शायद बिलकुल भी दिलचस्प आदमी मालूम नहीं होता था।
‘तुम यहाँ क्यों आने लगे?’ उसने पूछा।
‘दिल’ मैंने कहा, ‘मुझे सवेरे चहल-क़दमी बताई गई है। और आप? आपको क्या हुआ है?’
‘धुआँ’, उसने कहा, ‘मेरे मकान के आस पास होटल बहुत हैं। रात रहे से उनकी भट्टियाँ सुलगाई जाती हैं। उनका धुआँ मेरे लिए, मतलब मेरे फेफड़ों के लिए, ज़हर है।’
‘भट्टियाँ तो दिन भर जलती रहती हैं।’
‘दिन भर मैं बाहर रहता हूँ।’ वह रुका, फिर बोला, ‘नहीं, दिन भर तो वो जलती रहती हैं , लेकिन जब सुलगाई जाती हैं तो….’
अचानक उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने खड़े होकर थैले में हाथ डाला और कुछ निकालने की कोशिश की। फिर थैला मुझे पकड़ा कर दोहरा हो गया।
‘किसी और को भी बुला लो,’ उसने घुटी घुटी आवाज़ में कहा और ज़मीन पर बैठ गया।
मैंने दरख़्तों के झुंड में से निकल कर इधर उधर देखा। मैदान में अब कई बूढ़े टहल रहे थे लेकिन मुझे वो सब ख़ुद मदद के मोहताज मालूम हुए। मैं मैदान के दूर के हिस्सों तक गया। वहां भी कुछ बूढ़े लड़खड़ाते हुए टहल रहे थे। उनके मददगार भी एक तरफ़ बैठे हुए थे। मैंने देर तक उन में से एक को ग़ौर से देखा लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वह अपने अपने बूढ़े की जल्द ही वापसी के इन्तिज़ार में हैं इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और मायूस हो कर दरख़्तों के झुंड में वापस आ गया। मुझे याद नहीं आया कि मेरा दफ़्तरी साथी किस दरख़्त के नीचे था। मैंने आस पास के दरख़्तों के नीचे देख लिया। उसका कहीं पता नहीं था। मैंने शाहराह से मैदान को आने वाली कच्ची सड़क के दाहिने बाएं नज़र दौड़ाई। फिर शाहराह पर आ कर अपने मकान की तरफ़ चला। रास्ते भर मुझे यक़ीन रहा कि वह कहीं न कहीं धीरे धीरे चलता हुआ, या खड़ा हुआ, या बैठा हुआ या पड़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन वह किसी भी हालत में नहीं मिला और मैं अपने घर पहुँच गया।
घर पर जब मैं कपड़े बदल रहा था तो मैंने देखा उसका थैला अब भी मेरे हाथ में था।
2
कई दिन तक मैं मैदान के आस पास और शाहराह से कटने वाले दूसरे रास्तों पर उसे तलाश करता रहा। दो तीन बार झुंड के क़रीब आने पर मुझे शुबह हुआ कि वह अँधेरे में किसी दरख़्त के नीचे मौजूद है लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो दरख़्त के नीचे सिर्फ़ पत्तियों से टपकी हुई ओस थी। अपने पुराने दफ़्तरों में से जो मुझे याद रह गए थे, मैंने उनमें भी जाने का इरादा किया और दो दफ़्तरों में गया भी, लेकिन मैंने वहां सिर्फ़ दो दो चार चार महीने काम किया था। अब उनमें न कोई मेरा जानने वाला था, न मैं किसी को जानता था, न मेरी समझ में ये आया कि अपने उस साथी के बारे में किस तरह पूछ-ताछ करूँ जिसका मुझे न नाम याद था न ओहदा। आख़िर मैं इधर उधर की बातें पूछ कर चला आया और दफ़्तरों में उसे तलाश करने का ख़याल छोड़ दिया।
वह अब मैदान की तरफ़ नहीं जाता था। कम से कम उस वक़्त नहीं जाता था जब मैं वहां होता था। इस तरह उसको ढूंढ निकालने की मेरी कोशिशें बेकार गईं और इसका अजीब नतीजा ये निकला कि मैंने मैदान में जाना छोड़ दिया। इसी कैफ़ियत में एक दिन मेरी नज़र उसके थैले पर पड़ गई जो मेरे कपड़ों की अलमारी में रखा रह गया था। मुझे अपने आप पर हैरत हुई कि अभी तक मुझको थैले के सामान का जायज़ा लेकर उसके मालिक के पता चलाने का ख़याल नहीं आया था। मैंने थैले को मेज़ पर उलट दिया। उसमें कुछ मामूली रक़म के नोट थे, कुछ दवाएं थीं, कुछ रसीदें थीं जो अब ठीक से पढ़ने में नहीं आती थीं। दो तीन ख़त थे जो बहुत पहले के लिखे हुए मालूम होते थे और किसी ‘जनाब भाई साहब’ के नाम किसी ‘आपका ताबेदार अच्छन’ की तरफ़ से थे। लिफ़ाफ़ा किसी ख़त के साथ नहीं था, न ये मालूम होता था कि यह कब और कहाँ से और किस पते पर भेजे गए हैं। मैंने झिझकते झिझकते उन ख़तों को पढ़ डाला। लेकिन ये भी ‘छोटी ख़ाला’ और ‘मंझली फूफी साहब’ के बीमार या ख़ैरियत से होने की इत्तेला दे कर रह गए। एक किसी डेढ़ दो साल की बच्ची की तस्वीर भी थी जिसके पीछे लिखा हुआ था, ‘अमीना बिस्किट खा रही हैं।’ मैंने ये ज़ाती ख़त पढ़ने पर ख़ुद को मुजरिम महसूस किया और सामान के मालिक का फिर भी सुराग़ न मिला।
अब वह थैला मेरे सीने पर बोझ था। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि उसके मालिक का क्या हुआ होगा। वह मुझे जानता था, यह भी जानता था कि मैं मैदान में मिल सकता हूँ, लेकिन उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। क्या वह ज़िंदा या मुर्दा अपने घर पहुँच सका था? क्या उसे घर वालों ने तलाश किया था? क्या वह अपने घर में अकेला रहता था? क्या वह किसी गाड़ी के नीचे आ गया था और ला-वारिस लाश की तरह ठिकाने लगा दिया गया था? सवाल ही सवाल थे और मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। फिर मुझे यह वहशत-ज़दा कर देने वाला ख़याल आया कि मेरे पास एक ग़ायब हो जाने वाले आदमी का सामान है और इसके बारे में मुझसे पूछ-गछ हो सकती है। अगर वह किसी हादसे में किसी अनजान आदमी की वजह से मर गया है या अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है तो मुझको मुल्ज़िम ठहराया जा सकता है। उसके बाद तरह तरह के अंदेशों ने मुझे घेर लिया और हर अंदेशा पुलिस, जिरह और हवालात तक पहुँचता था। मेरी ज़िन्दगी यूँ भी कुछ अच्छी नहीं गुज़र रही थी। लेकिन एक मुल्ज़िम बल्कि मुजरिम की सी ज़िन्दगी का ख़याल मेरी बर्दाश्त से बाहर था। जब ये ख़याल मुझ पर हर वक़्त मुसल्लत रहने लगा तो एक दिन मैंने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर के थैले को निकाला। यह हाथ के करघे पर बने हुए कपड़े का मज़बूत और नया थैला था। मुझे बहुत पसंद आया। थैले के अंदर के सामान को मैंने बाहर निकाल कर देखा और वापस थैले में रख दिया और बहुत सी आग जलाई। शुरू में उसका धुआँ मेरा दम घोंटने लगा, फिर शोले भड़क उठे। मैंने थैले को आग में डाल दिया और जब तक वह बिलकुल राख नहीं हो गया, एक लकड़ी से उसे उलटता पलटता रहा। इस तरह जनाब, भाई साहब और ताबेदार अच्छन और छोटी ख़ाला और मंझली फूफी साहिबा और अमीना और उसका बिस्किट और दवाएँ और वह रक़म और रसीदें नाबूद हो गईं। मेरा ख़याल है सबसे बाद में अमीना का बिस्किट जल कर राख हुआ।
जब मैं राख को समेट रहा था तो मुझको ऐसा मालूम हुआ कि अब वाक़ई मैंने उस शख़्स को मार डाला है। इस ख़याल ने मुझे कम तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, लेकिन फिर मैं ऐसे मुजरिम की तरह मुत्मइन हो गया जिसने अपने सारे जुर्म के सुबूत ज़ाए कर दिए हों।
3
कुछ दिन तक मुझे उसका ख़याल सताता रहा। यह ख़याल भी कई बार आया कि मुझको उसका थैला जलाना नहीं चाहिए था, हो सकता है वह ज़िंदा हो। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ मैं उसे भूल भाल गया। इस दौरान एक बार मेरी डॉक्टरी जांच भी हुई। दिल की ख़राबी कुछ कम हो गई थी। चहल क़दमी को पूछा गया तो मैंने बता दिया अब भी करता हूँ, लेकिन इससे मेरी मुराद ये थी कि रोज़ घर से बाहर निकलता हूँ। लेकिन मेरे बाहर निकलने का कोई वक़्त तय नहीं था। जब भी जी चाहता, निकल खड़ा और इधर उधर आवारा-गर्दी करके वापस आ जाता।
एक दिन मेरा गुज़र एक ऐसे मोहल्ले में हुआ जो शहर में मशहूर था लेकिन मैं उधर कभी नहीं आया था। ये एक बड़े बाज़ार के बाद पड़ता था और उसके बाद एक और कारोबारी इलाक़ा शुरू हो जाता था। उस मोहल्ले में गलियाँ बहुत थीं। मैं उन गलियों में भटक रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी गली मुझे मोहल्ले से बाहर ले जा सकती है। एक गली से दूसरी गली में जा रहा था कि सामने से आते हुए एक आदमी ने मुझे देखा और ठिठक कर रुक गया। मैं भी उसके क़रीब पहुँच कर रुक गया।
‘अरे, तुम?’
‘तुम?” मैंने भी कहा और हम दोनों गले लग गए।
वह मेरे स्कूल के दिनों का गहरा दोस्त था। इतने दिन बाद भी हमें एक दूसरे को पहचानने में दिक़्क़त नहीं हुई। वहीं खड़े खड़े हमने अपनी मौजूदा ज़िन्दगी, फिर स्कूल की बातें शुरू कर दीं। पुराने मास्टरों का ज़िक्र आया, पुराने साथियों का हाल मालूम किया गया और अपनी शरारतें याद आईं। वह बहुत ज़िंदा दिल लड़का था। अब भी उसकी बातों में शोख़ी झलक जाती थी। मुझको उसका अचानक मिल जाना अच्छा मालूम हुआ। वह गाता भी बहुत था और उस वक़्त मशहूर गानों की नक़ल अच्छी कर लेता था। लेकिन कोई गाना पूरा नहीं गाता था। एक गाना शुरू करता और एक दो बोलों के बाद उसमें किसी दूसरे गाने का जोड़ मिला देता, फिर तीसरे गाने का। इसी तरह पंद्रह बीस गाने सुना देता। कोई उससे पूरा गाना सुनाने की फ़रमाइश करता तो कह देता था, ‘पूरा याद नहीं।’ और सच्ची बात यह है कि हमको उससे अधूरे गाने सुनने ही में मज़ा आता था। मैंने उसके गानों का ज़िक्र छेड़ दिया और पूछा :
‘अब भी पैवंदी गाने गाते हो?’
‘अब कहाँ, मेरी आवाज़ देख रहे हो?’ उसने कुछ उदास हो कर कहा और चुप हो गया।
वाक़ई उसकी आवाज़ ख़राब हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा :
‘इतने दिन बाद मिले हो। आओ थोड़ी देर बैठते हैं। क़रीब ही मकान है।’
हम एक और गली में दाख़िल हुए। थोड़ा चलने के बाद वह एक छोटे से होटल के सामने रुका और होटल वाले से कुछ कह कर आगे बढ़ा। तीन चार होटल एक दूसरे से मिले हुए थे। फिर उसका मकान आ गया। दाख़ले का दरवाज़ा छोटा था लेकिन अंदर कुशादा मकान था। सहन भी था। दरवाज़े के क़रीब एक कमरे में हम दोनों बैठे एक दूसरे को अपना अपना हाल बता रहे थे कि किसी ने बाहर का दरवाज़ा खटखटाया। दोस्त ने आवाज़ दी :
‘चले आओ!’
एक छोकरा सिर्फ़ जांघिया पहने, हाथों में चाय के दो ग्लास और दो तश्तरियाँ लिए हुए दाख़िल हुआ। मुझे कुछ हैरत हुई कि उसने दो हाथों में चार चार चीज़ें संभाल रखी हैं। सब सामान उसने एक मेज़ पर रखा और दौड़ता हुआ वापस चला गया।
उस वक़्त हम अपने मास्टरों को दिए नाम याद कर कर के हंस रहे थे।
‘मास्टर तबला याद हैं?’ उसने पूछा।
‘उन्हें भी कोई भूल सकता है?’
वह हमारे मास्टरों में सबसे सीधे थे। अगर किसी लड़के पर उनको बहुत ग़ुस्सा आता तो दोनों हाथों से उसकी पीठ पर आहिस्ता से तबला सा बजा देते थे, बस।
‘उनका कोसना भी याद है?’
‘नहीं,’ मैंने कहा, ‘क्या वह कोसते भी थे?’
‘एक बार मैं घर से काम कर के नहीं ले गया था। उन्होंने बार बार पूछा, ‘काम क्यों नहीं कर के लाया?’ मेरे पास जवाब नहीं था, चुपका खड़ा रहा। उन्होंने कहा, ‘बोलता क्यों नहीं? बोल नहीं तो कोसता हूँ।’ मैं फिर चुप रहा। कहने लगे, ‘नहीं बोलेगा? तो कोसूं?’ फिर पूछा, ‘कोसूं?’ मैंने कहा, ‘कोसिये।’ तो बोले ‘मुर्दा लड़का!’ मुझे ये कोसना सुन कर हंसी आ गई।’
‘फिर?’ मैंने हँसते हुए पूछा।
‘फिर क्या। अब उनको असली ग़ुस्सा आया और उन्होंने मेरी पीठ पर तबला बजा दिया। स्कूल छोड़ने के बहुत दिन बाद एक बार उनसे मुलाक़ात हुई। उन्हें सांस की शिकायत हो गई थी। यार, हमारा मकान बड़ा वाहियात है।’
उसने एक बात में दूसरी बात का जोड़ लगा दिया, जिस तरह गानों में लगाया करता था। मैंने कहा :
‘क्यों? वाहियात क्यों? इतना अच्छा तो मकान है।’
‘हाँ, लेकिन यहाँ होटल बहुत हैं।’
मेरे दिमाग़ में घंटी सी बजने लगी। मैंने कहा :
‘होटल हैं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं? खाने पीने की आसानी रहती होगी।’
उसने वही कहा जो मैं सुनने की उम्मीद कर रहा था। बोला :
‘वो तो ठीक है, लेकिन अँधेरे में इनकी भट्टियाँ सुलगाई जाती हैं। सारे में धुआँ फैल जाता है। मेरा तो दम घुटने लगता है। और मैं समझता हूँ मेरी आवाज़ इसी से ख़राब हुई है।’
मैं चाहता तो इस गुफ़्तगू को आगे बढ़ा सकता था लेकिन अचानक मुझे उस थैले का ख़याल आया जिसे मैंने जला दिया था।
कोई फ़ायदा नहीं, मैंने सोचा और उठने को हुआ, लेकिन उसी वक़्त दोस्त ने कहा :
‘पड़ोस में एक साहब रहते थे। वह तो भट्टियाँ सुलगने से पहले घर से बाहर निकल जाते थे। मालूम नहीं कहाँ जाते थे। सूरज निकलने के वक़्त वापस आते थे। लेकिन इस तरह कब तक काम चल सकता था।’
अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने पूछा :
‘तो अब नहीं निकलते?’
‘नहीं, एक दिन बिलकुल ही निकल गए। उनके मकान से मिला हुआ एक और होटल खुल गया है। है ना मज़े की बात?’ फिर उसे कुछ याद आया। बोला, ‘अरे हाँ, वह उनका थैला…क्या नाम था उनका?’
‘कैसा थैला?’ मैंने ब-मुश्किल कहा।
‘वह किसी वक़्त भी उनसे अलग नहीं होता था। हम लोगों के साथ क्रिकेट मैच खेलते वक़्त भी उनके कंधे से लटका रहता था।’
मुझे याद आ गया।
‘अच्छा वह?’ मैंने कहा। ‘हाँ वह ड्राइंग मास्टर। एक बार रन लेने के लिए दौड़े, आधे रास्ते में थैला गिर गया तो उठाने के लिए रुक गए और…’
‘रन आउट हो गए!’ उसने कहा और ज़ोर से क़हक़हा लगाया। मैं भी हंसने लगा। कुछ देर हम ड्राइंग मास्टर की बातें करते रहे। फिर मैं उठ खड़ा हुआ। चलते चलते मैंने कहा :
‘एक बात बताओ।’
‘बोलो बोलो।’
‘कई गलियों में होता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। बाहर जाने का रास्ता कौनसा है?’
‘बस?’ वह हंसा, ‘यही सामने वाली गली है। सीधे आगे बढ़ते जाओ। कहीं मुड़ना मत। गली अपने आप तुम्हें बाज़ार में पहुँचा देगी। या चलो मैं तुम्हारे साथ सड़क तक चलता हूँ।’
गली के सिरे पर पहुँच कर वह फिर मुझसे गले मिला और बोला :
‘यार, कभी कभी आ जाया करो।’
‘ज़रूर आऊंगा।’ मैंने कहा और सड़क पर आ गया।
कुछ क़दम बढ़ने के बाद मैंने पीछे मुड़ कर देखा। वह गली में मुड़ रहा था। उसका मकान मुझे याद था लेकिन यक़ीन था कि दो दिन बाद याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं पलट कर उसके पीछे चला। वह मकान में दाख़िल हो रहा था कि मैंने उसे जा लिया। वह कुछ हैरान होकर मुझे देखने लगा। मैंने कहा :
‘यार, एक बात पूछना भूल गया था।’
‘हाँ हाँ, कहो।’
फिर मुझे झिझकते देख कर बोला :
‘आओ कुछ देर और बैठते हैं। कितने दिन बाद तो मुलाक़ात हुई है।’
कमरे में कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद उसने कहा :
‘तुम कुछ पूछ रहे थे।’
‘हाँ,’ मैंने कहा, ‘वो….तुम कह रहे थे एक और होटल खुल गया है।’
‘होटल तो खुलते ही रहते हैं,’ वह बोला, ‘और बंद भी होते रहते हैं।’
‘नहीं,’ मैंने कहा, उनके मकान से मिला हुआ…जो साहब धुएँ की वजह से….’
अच्छा, मलिक साहब को पूछ रहे हो?’
और मुझे भी उसका नाम याद आ गया।
‘मलिक साहब,’ मैंने कहा, ‘उनके साथ कुछ दिन दफ़्तर में काम किया था। दो तीन बार उनके घर भी आया था।’ हालांकि नहीं आया था। ‘वह मुझ पर बहुत मेहरबान थे। मैं भी उनसे बे-तकल्लुफ़ था।’
फिर मैंने उसकी मेहरबानियों और अपनी बे-तकल्लुफ़ी के कई क़िस्से भी गढ़ कर सुआए। मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे इतने बहुत से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। दोस्त ने मेरी बातों को दिलचस्पी के बग़ैर सुना, फिर बोला :
‘हाँ, वह सीधे सादे आदमी थे, और मैं समझता हूँ कुछ कुछ सनकी भी थे।’
‘सनकी?’
‘या शायद न हों – लेकिन उनका थैला…’ वह रुका, फिर बोला, ‘थैला हर वक़्त उनके पास रहता था।’
‘हमारे ड्राइंग मास्टर की तरह?’
‘ड्राइंग मास्टर तो जब उनका थैला ख़राब हो जाता था, तब बदलते थे। मलिक साहब हर दूसरे तीसरे महीने नया थैला ख़रीदते थे। ये सनक ही तो थी एक क़िस्म की।’
‘उनके बीवी बच्चे?’
‘कहीं और हों तो हों। यहाँ अकेले ही रहते थे। आख़िर में उनका शायद कोई दोस्त भी नहीं था।’
‘तुम भी नहीं?’
‘मेरी उनसे बस कुंजी भर की दोस्ती थी।’
उसने बताया कि सवेरे घूमने जाते वक़्त वह अपने दरवाज़े की कुंजी उसके दरवाज़े पर लटका जाता था और वापस आ कर उतार लेता था।
‘उस दिन दोपहर तक कुंजी यूँही लटकती रही। तीसरे पहर के क़रीब एक आदमी उनकी ख़बर लेकर आ गया। रेलवे मैदान में टहलने जाते थे। वहीं ख़त्म होगए।’
फिर दोस्त ने विस्तार से बताया कि मैदान में टहलने वालों को दरख़्तों के झुंड में किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी लेकिन जब तक लोग आवाज़ पर पहुँचे वह बेहोश हो चुका था। इत्तिफ़ाक़ से उनमें दो लोग ऐसे थे जो कभी उसके साथ दफ़्तर में काम कर चुके थे। उन्होंने उसे पहचाना, हस्पताल ले गए। हस्पताल में बताया गया कि वह मर चुका है। उसके दफ़्तर में ख़बर भेजी गई। दफ़्तर वालों ने अपने पुराने रिकॉर्ड में उसके घर का पता देख कर मोहल्ले वालों को ख़बर की और मोहल्ले वाले हस्पताल और पुलिस से निपट कर उसकी लाश ले आए।
‘बे-वक़्त मरना,’ मैंने आहिस्ता से कहा।
‘अगर वहां टहलने वालों में कोई शनासा न निकलता तो मालूम नहीं बे-चारे का क्या हश्र होता।’
मैंने ला-वारिस लाशों के हश्र का तसव्वुर किया, फिर उधर से ध्यान हटा कर पूछा :
‘तो वह उसी झुंड में मिले?’
‘वह शायद उसी में से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग़लती से झुंड के अंदर तक चले गए।’
‘ये किस तरह कह रहे हो?’
‘उनके थैले की वजह से। जहाँ पर वह पाए गए, वहां थैला नहीं था। कहीं दरख़्तों में गिर गया होगा।’
‘हो सकता है उस दिन थैला न ले गए हों।’
‘कोई सवाल नहीं। थैला हर वक़्त उनके पास रहता था। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई और उन्होंने दरख़्तों में से निकलना चाहा तो रास्ते में कहीं उनके हाथ से छूट गया होगा।’
‘मगर वह नहीं मिला?’
‘किसी ने पार कर दिया होगा, नया थैला था। या शायद अब भी कहीं दरख़्तों में पड़ा हो।’
मैंने बात बदलने के लिए कहना शुरू किया :
‘उनके घर वाले…’
‘बताया ना, वह अकेले रहते थे। लेकिन उन्होंने पड़ोस के दो होटल वालों को रूपए दे रखे थे कि उन्हें कुछ हो जाए तो…’
फिर उसने कफ़न दफ़न, क़ब्रिस्तान का ज़िक्र छेड़ दिया जो मैंने कुछ सुना, कुछ नहीं सुना। उसके बाद हम फिर इधर उधर की बातें करने लगे। आख़िर मैं उठ खड़ा हुआ। दोस्त ने फिर कहा :
‘यार, कभी कभी आ जाया करो।’
‘देखो, अगर गलियाँ याद रह गईं।’
उसने सड़क से अपने मकान तक की निशानियाँ बताना शुरू कीं, फिर उसे कुछ याद आया, बोला :
‘अरे भाई, मलिक साहब का मकान तो जानते हो, बस उसके बाएं तरफ़ तीसरा मकान… ‘
मैंने कहा :
‘तुम भी कभी कभी आ जाया करो।’
मैंने उसे अपना पता नहीं बताया, इसलिए कि मेरा मकान स्कूल के रास्ते में पड़ता था और हम अक्सर दरवाज़े पर खड़े हो कर बातें किया करते थे।
मैं वहां से चला आया। कुछ दिन तक सोचता रहा कि अगर उसे दरख़्तों के झुंड ही में तलाश करता तो शायद वह बच जाता, लेकिन फिर उसको, और अपने दोस्त को भी, भूल भाल गया।
4
अब बे-वक़्त मरने का डर मेरे दिल से निकल गया था, इसलिए कि एक बार फिर मेरी डॉक्टरी जांच हुई तो दिल की हालत ठीक ठाक निकली जिसके बाद मैंने बाहर निकलना बहुत कम कर दिया। ज़्यादा-तर अपने छोटे से बाग़ के पेड़-पौधों या घर में पली हुई मुर्ग़ियों की देख-भाल करता था।
एक दिन मैं मोहल्ले की चक्की पर मुर्ग़ियों का दाना लेकर आ रहा था कि देखा वह मेरा दोस्त मेरे मकान की तरफ़ से चला आ रहा है। क़रीब आते ही बोला :
‘ख़ूब मिले। मैं वापस जा रहा था।’
‘बस ज़रा देर के लिए बाहर निकला था। आओ, बैठते हैं।’
‘बैठूंगा नहीं,’ उसने कहा। ‘इस वक़्त ये बताने आया हूँ कि वह लोग, मलिक साहब के घर वाले, आ गए हैं।’
‘तो मैं क्या करूँ?’
‘मैं क्या करूँ?’ उसने मेरी बात को दोहराया और ज़ोर से हंसा, ‘याद है?”
मुझे याद आया। स्कूल के दिनों में हमारी एक तफ़रीह यह भी थी कि अपने किसी साथी से किसी दिलचस्प ख़बर की तफ़सील पूछते और जब वह बहुत जोश के साथ बता चुकता तो रूखा मुंह बना कर कह देते, ‘तो मैं क्या करूँ?’
‘हाँ, याद है,’ मैं भी हंसने लगा, ‘लेकिन मलिक साहब के घर वाले आ गए हैं तो मैं वाक़ई क्या करूँ?’
‘भई वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं।’
‘मुझसे क्यों?’
‘तुम मलिक साहब से बे-तकल्लुफ़ थे ना? वो लोग उनके मिलने वालों से मिल रहे हैं।’
‘मेरी उनसे ज़्यादा मुलाक़ात नहीं थी। बस दफ़्तर के दिनों में…’ फिर मैं रुक गया।
‘चलो, जो कहना है, उन्हीं से कहना। वो लोग आज वापस जा रहे हैं।’
‘और आए कब थे?’
‘कई दिन हो गए। आज मैंने उनसे तुम्हारा ज़िक्र किया तो….’
मैंने दिल ही दिल में उसे कोसा, दाने की पोटली घर में पहुँचाई, और उसके साथ चल दिया।
रास्ते में उसने मुझे बताया कि वो लोग किसी दूसरे मुल्क में बस गए हैं और यहाँ अपने रिश्तेदारों से उनका राब्ता नहीं रह गया था। ‘बल्कि मलिक साहब के सिवा कोई रिश्तेदार ही नहीं रह गया था।’ मलिक साहब से उनका क्या रिश्ता था, ये उसे मालूम नहीं था।
हम वहां पहुँच गए। मकान कुछ कुछ वैसा ही था जैसा मेरे दोस्त का मकान था। मेहमानों की वजह से वहां बड़ी चहल-पहल थी। उनमें दो नौजवान थे, एक मियाँ बीवी थे, ये भी जवान ही थे, एक अधेड़ उम्र की औरत थी और दो एक बच्चे थे। लिबासों और साथ के सामान से ख़ासे ख़ुश-हाल लोग मालूम होते थे। दोस्त ने मेरा तार्रुफ़ कराया और मैं उनके सवालों के लिए तैयार होगया जिनके जवाब रास्ते भर सोचता आ रहा था। लेकिन उन लोगों ने बस सरसरी तौर पर मेरे बारे में कुछ सवाल किये। कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ वग़ैरह। उनको मेरे जवाबों से दिलचस्पी नहीं मालूम होती थी। ज़्यादातर वो अपने बारे में मुझको बताते रहे। अधेड़ औरत मेरे दोस्त से धीरे धीरे बातें करती रही। मैं नौजवानों से बात कर रहा था लेकिन उनकी बातें ध्यान से सुन नहीं पा रहा था। बस इतना समझ में आया कि उन्होंने मकान के लिए ख़रीदार का इंतिज़ाम कर लिया है, घर का सामान ठिकाने लगा चुके हैं, और यह कि शाम को उनकी वापसी है और जाने से पहले वह शहर की तारीख़ी इमारतें देखेंगे।
मैंने दोस्त को वापस चलने का इशारा किया और हम दोनों उठ खड़े हुए। अधेड़ औरत अभी तक दोस्त से बातें कर रही थी। उसके आख़री जुमले मुझे याद हैं :
‘मुझे तो वह याद भी नहीं हैं। अच्छन भाई के पास उनके ख़त देखे थे। बड़ी मोहब्बत से लिखते थे,’ उसने ठंडी सांस भरी। ‘उनके सामान में हम लोगों के खिलौने भी निकले। अभी तक उन्हें संभाल कर रखे हुए थे।’
०००
नैयर मसूद 1936 में पैदा हुए और 2017 में उनका इन्तिक़ाल हुआ। उनका तअल्लुक़ लखनऊ शहर से था। उनकी कहानियों की किताबों में ‘गंजिफ़ा‘, ‘इत्र-ए-काफ़ूर‘ और ताऊस चमन की मैना‘ के अलावा और भी कहानी संग्रह, मीर अनीस की जीवनी और फ़ारसी कहानियों के उर्दू अनुवाद शामिल हैं. काफ़्का की कहानियों के भी कुछ तर्जुमे उन्होंने किये हैं। वह उर्दू कहानी का बेहद अहम नाम हैं।
नैयर मसूद की कुछ कहानियाँ हिंदी में आ चुकी हैं, मगर ज़्यादा तर कहानियों का अनुवाद या लिप्यंतरण कुछ कमज़ोरियों का शिकार रहा है। इसलिए चाहता हूँ कि उनकी कहानियों के लिप्यंतरण पर ख़ुद काम करूँ। इस कहानी का नाम है दुंबाला-गर्द, जिसका मतलब होता है पीछा करने वाला, पीछे पीछे फिरने वाला। उनके फ़िक्शन की सबसे ख़ास बात ये है कि वह बड़े सरल सजल अंदाज़ में कहानी को तराशते चले जाते हैं। ज़िन्दगी की तरह कहानी भी किसी मक़सद या तहरीक के फेर में पड़े बिना पेचदार गलियों से गुज़रती है और आख़िर में कहीं धुंधलाती हुई ग़ायब हो जाती है। नैयर साहब उर्दू में जदीद या नई कहानी की राह पर किसी राहनुमा की तरह हर नए उर्दू लेखक को कहानी के हुनर को बरतने का सलीक़ा सिखाते भी मालूम होते हैं। लिप्यंतरण या अनुवाद में अगर कहीं कोई कमज़ोरी महसूस हो तो दोस्त ज़रूर बताएं। शुक्रिया!