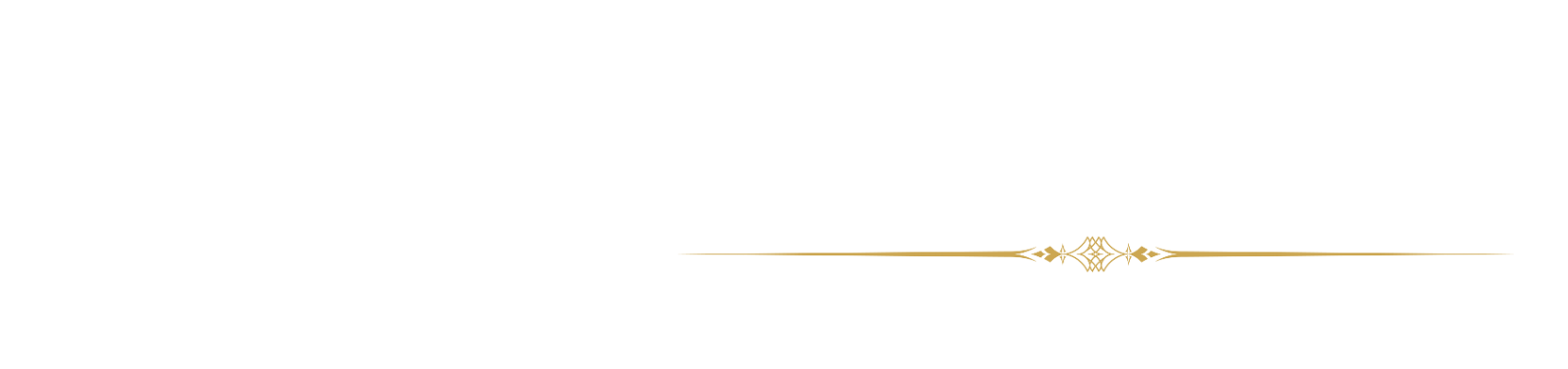समय का बंधन
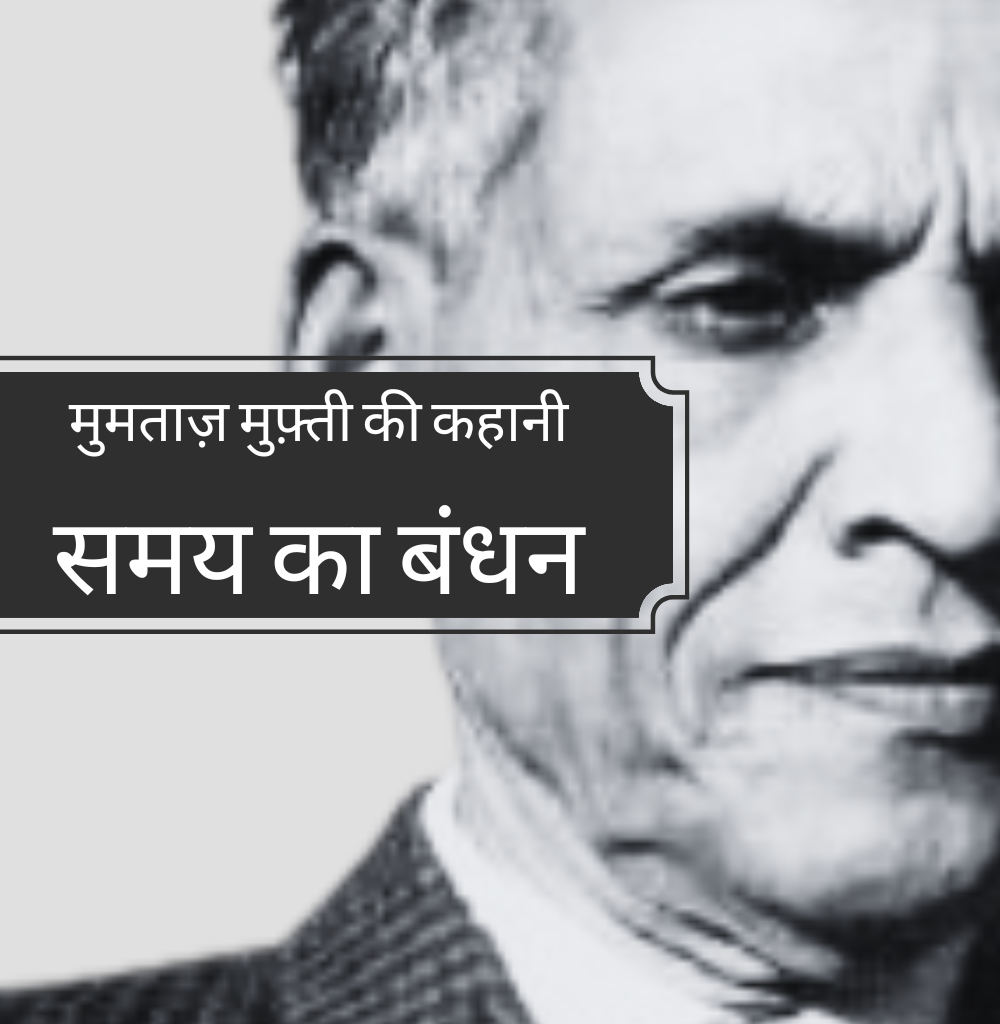
आपी कहा करती थी, सुनहरे, समय समय की बात होती है। हर समय का अपना रंग होता है, अपना असर होता है। अपने समय पहचान, सुनहरे। अपने समय से बाहर न निकल। जो निकली तो भटक जाएगी।
अब समझ में आई आपी की बात। जब समझ लेती तो रस्ते से न भटकती। आलने से न गिरती, समझ तो गई। पर कितनी क़ीमत देनी पड़ी समझने की। आपी मुझे सुनहरे कह कर बुलाया करती थी। कहती थी तेरे पिंडे की झाल सुनहरी है। जब रस आएगा तो सोना बन जाएगी, कठाली में पड़े बिना। फिर ये झाल कपड़ों से निकल-निकल कर झाँकेगी।
पता नहीं मेरा नाम क्या था। पता नहीं मैं किस की थी, कहाँ से आई थी। कोई लाया था। बालपन ही में आपी के हाथ बेच गया था। उसी की गोद में पली। उसी की सुर-ताल भरी बैठक के झूलने में झूल-झूल कर जवान हुई। फिर सुनहरा उमड़-उमड़ आया। छुपाए न छुपता था। आपी बोली, न धिये, छुपा न। जो छुपाए न छुपे उसे क्या छुपाना।
कभी खिड़की से झाँकती तो आपी टोकती, “ये क्या कर रही है बेटी? सयाने कहते हैं, जिसका काम उसी को साझे। तेरा काम देखना नहीं। दिखना है। तू नज़र न बन, मंज़र बन और जो देखे भी तो तू दिखने का घूँघट निकाल। उसकी ओट से देख। फिर समय देख सुनहरे। अभी तो शाम है। ये समय तो उदासी का समय है। दुख का समय है। शाम भई घनशाम न आए।” आपी गुनगुनाने लगी, “याद है न ये बोल? शाम तो न आने का समय है। तेरा आने का समय है। पगली ज़रा रुक जा। अंधेरा गाढ़ा होने दे। फिर तेरा ही समय होगा। पिछले-पहर तक।”
एक दिन आपी का जी अच्छा न था। मुझे बुलाया। गई, लेटी हुई थी। सिरहाने तिहाई सोडे की बोतल धरी थी। साथ नमकदानी थी। ये उन दिनों की बात है जब सोडे की बोतल के गले में शीशे का गोला फंसा होता था। ‘ठा’ करके खुलता था। बोली, “सुनहरे, बोतल खोल, गिलास में डाल। चुटकी भर नमक घोल और मुझे पिला दे।” मैंने नमक डाला तो झाग उठा। बुलबुले ही बुलबुले। आपी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोली, “देख लड़की, ये हमारा समय है। हमारा समय वो है जब झाग उठे। हम में नहीं। दूजे में उठे। दूजे में झाग उठाना यही हमारा काम है। ख़ुद शांत दूजा बुलबुले ही बुलबुले। और जब समय बीत जाए तो धीरज पाँव धरना। ठुमक न करना। ठुमक का समय गया। चमक न मारना। चमक का समय गया। पायल न झंकारना। पायल की झंकार बैरन भई।”
फिर वो लेट गई। बोली, “सुनहरे, मेरी बातें फेंक न देना। दिल में रखना। ये भीतर की बातें हैं, ऊपर की नहीं, सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं। वो सब छिलके होते हैं, बादाम नहीं होते। जान ले बेटी बात वो जो भीतर की हो। गिरी हो, छिलका न हो। जो बीती हो। जग-बीती नहीं। आप-बीती हो। हड्ड बीती। बाक़ी सब झूट। दिखलावा। बहलावा।”
आज मुझे बातें याद आ रही हैं। बीती बातें। बिसरी बातें। साँप गुज़र गए। लकीरें रह गईं। लकीरें ही लकीरें। साँप तो सिर्फ़ डराते हैं। फुंकारते हैं। लकीरें काटती हैं। डसती हैं, पता नहीं, ऐसा क्यों होता है। लकीरों ने मुझे छलनी कर रखा है। चलती हैं। चले जाती हैं। जैसे धार चलती है। एक ख़त्म होती है दूजी शुरू हो जाती है।
आपी की बैठक में हम तीन थीं। पीली, रूपा और मैं। पीली बड़ी, रूपा मंझली और मैं छोटी। पीली में बड़ी आन थी। पर मान न था। उस आन में छब थी। सुंदरता भरा ठहराओ था। यूँ रौब से भरी रहती जैसे मुटियार रस भरी रहती है। मूर्ती समान।
रूपा सुर ही सुर थी। तारों से बनी थी। उस के बंद-बंद में तार लगे थे। सुरतियाँ स्मृतियाँ। और वो गूँजते मद्धम में गूँजते और फिर सुनने वालों के दिलों को झुला देते। तीजी मैं थी। आपी कहती थी, सुनहरे, तुझ में दुख की भीग है। तू भिगो देती है। ख़ुद भी डूब जाती है दूजे को भी डुबो देती है। पगली दूजे को डुबोया कर, ख़ुद न डूबा कर। मुझे तुझ से डर आता है सुनहरे। किसी दिन तू हम सबको न ले डूबे।
आपी की बैठक कोई आम बैठक न थी कि जिस का जी चाहा मुँह उठाया और चला आया। बैठक पर धन-दौलत का ज़ोर तो चलता ही है, बैठक पर आपी ने बरताव का ऐसा रंग चला रखा था कि ख़ाली धन-दौलत का ज़ोर न चलता था। नौ दौलतिये आते थे। पर ऐसे बदमज़ा हो कर जाते कि फिर रुख़ न करते। आपी की बैठक में निगाहें नहीं चलती थीं। उसने हमें समझा रखा था कि लोग निगाहों पर उछालेंगे तो पड़े उछालें। लड़कियो तुम न उछलना। जो निगाहों पर उछल जाती हैं वो मुँह के बल गिरती हैं। और जो गिर गई वो समझ लो, नज़रों से गिर गई। फिर न अपने जोगी रही न दूसरों जोगी।
आपी की बैठक में नज़रें नहीं चलती थीं। कान लगे रहते थे। दिल धड़कते थे। वहाँ मिलाप का रंग न होता था। बिरहा का होता। रंग-रलियाँ नहीं होती थीं। न वहाँ तमाशा होता न तमाशबीन।
मुझे वो दिन याद आते हैं जब हमारे हाँ ठाकुर बैठक लगती थी। दो महीने में एक बार ज़रूर लगती थी। ठाकुर की बैठक लगती तो कोई दूजा नहीं आ सकता था। सिर्फ़ ठाकुर के संगी साथी।
ठाकुर भी तो अजब था। ऊपर से देखो तो रीछ। ताक़त से भरा हुआ। अंदर झाँको तो बच्चा। नर्म-नर्म, गर्म-गर्म। वैसे था आन भरा। संगत का रसिया। यूँ लगता जैसे भीतर कोई लगन लगी हो। धूनी रमी हो। आरती सजी हो। ठाकुर की हमारे हाँ बड़ी क़दर थी। आपी इज़्ज़त करती थी। भरोसा करती थी। ठाकुर ने भी कभी नज़र उछाली न थी। झुकाए रखता। पीता ज़रूर था, पर ऐसी कि जूँ-जूँ पीता जाता उल्टा मद्धम पड़ता जाता। आँख की चमक गुल हो जाती। आवाज़ की कड़क भीग जाती। उसका नशा ही अनोखा था। जैसे बोतल का न हो, भीतर का हो। बोतल एक बहाना हो। बोतल चाबी हो भीतर के पट खोलने की।
डरो सखियो डरो। भीतर के नशे से डरो। भीतर के नशे के सामने बोतल का नशा यूँ हाथ जोड़े खड़ा है जैसे राजा के रू-ब-रू नीच खड़ा हो। बोतल का ख़ाली सर चकराता है। भीतर का मन का झूलना झुला देता है। डरो सखियो डरो भीतर के नशे से डरो। बोतल का तो काम काज जोगा नहीं छोड़ता। भीतर का किसी जोगा नहीं छोड़ता। ख़ुद जोगा भी नहीं। मुझे क्या पता था कि ठाकुर के नशे का रेला मुझे भी ले डूबेगा।
हाँ, तो उस रोज़ ठाकुर की बैठक हो रही थी। बोल थे, गाँठरी मैं कौन जतन कर खोलूँ। मोरे पिया के जिया में पड़ी रही। गीत ने कुछ ऐसा समाँ बाँध रखा था कि ठाकुर झूम-झूम जा रहा था। फिर कहो, फिर बोलो का जाप किए जा रहा था। न जाने किस गिरह को खोलने की आरज़ू जागी थी। अपने मन या महबूब के मन की। समय बीता जा रहा था। समय की सुध-बुध न रही थी। कभी-कभी ऐसा भी होता है। समय जीवन से निकल जाता है कि कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। किसी बात की सुध-बुध नहीं रहती। उस रोज़ वो समय ऐसा ही समय था।
दफ़्अतन घड़ी ने तीन बजाए। आपी हाथ जोड़े उठ बैठी। बोली, “शमा करो, ठाकुर जी। माफ़ी माँगती हूँ, हमारा समय बीत गया। अब बैठक ख़त्म करो।” ठाकुर पहले तो चौंका, फिर मुस्काया, “न आपी वो बोला, अभी तो रात भीगी है। आपी बोली, ठाकुर हम सूखे परों वाले पंछी हैं। जब रात भीग जाती है तो हमारा समय बीत जाता है। जो हमारे पर भीग गए तो उडारी न रहेगी। फ़नकार में उडारी न रहे तो बाक़ी रहा क्या?” ठाकुर ने बड़ी मिन्नतें कीं। आपी न मानी। महफ़िल टूट गई तो हम तीनों आपी के गिर्द हो गईं। “आपी, ये समय का गोरख धंदा क्या है?”
आपी बोली, “लड़कियो समय बड़ी चीज़ है। हर काम का अलग समय बना है। रात को गाओ बजाओ, पियो-पिलाओ, मिलो-मिलाओ, मौज उड़ाओ। बस तीन बजे तक। फिर भोर समय उस का समय है। उस का नाम जपो, उसे पुकारो, फ़रियाद करो, दुआएँ माँगो, सज्दे करो। उस समय में तुम ऐश नहीं कर सकते। गुनाह नहीं कर सकते। क़त्ल नहीं कर सकते। ये धंदा जो हमारा है उस के समय में नहीं चल सकता। उस के समय में पाँव न धरना। उस ने बुरा माना तो मारी जाओगी। जो वो राज़ी हो गया तो भी मारी जाओगी। और देखो उस के समय के नेड़े-नेड़े भी ऐसा गीत न गाना जो उसे पुकारे। भजन न छेड़ना। डरो, कहीं वो तुम्हारी पुकार सुन कर हुंकारा न भर दे।”
फिर वो दिन आ गया जब मैंने अनजाने में समय का बंधन तोड़ दिया। उस रोज़ ठाकुर आए। आपी से बोले, “बाई कल ख़्वाजा का दिन है। ख़्वाजा की नियाज़ सारे गाँव को खिलाऊँगा। आज रात ख़्वाजा की महफ़िल होगी उधर हवेली में। सिर्फ़ अपने होंगे, घर के लोग। तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ मेरे गाँव।”
“आपी सोच में पड़ गई। बोली, रूपा माँदी है। वो तो नहीं जा सकेगी। किसी और दिन रख लेना नज़र-नियाज़।”
“ख़्वाजा का दिन मैं कैसे बदलूँ?” वो बोला।
“तो किसी और मंडली को ले जा।”
“ऊँहूँ!” ठाकुर ने मुँह बना लिया, “ख़्वाजा की बात न होती तो ले जाता। उन का नाम लेने के लायक़ मुख तो हो।”
“मैं किस लायक़ हूँ जो उन का नाम मुँह पर लाऊँ।”
“बस इक तेरी ही बैठक है बाई जहाँ पवित्रता है। जहाँ जिस्म का नहीं मन का ठिकाना है।”
आपी मजबूर हो गई। उसने रूपा का ध्यान रखने के लिए पीली को वहाँ छोड़ा और मुझे लेकर ठाकुर के गाँव चली।
रात भर वहाँ हवेली में ख़्वाजा की महफ़िल लगी। वो तो घरेलू महफ़िल थी। ठाकुर की बहनें, बहुएँ, बेटियाँ, ठाकुरानी सब बैठे थे। वो तो समझ लो भजन मंडली थी और ख़्वाजा के गीत, ख़्वाजा मैं तो आन खड़ी तोरे द्वार से शुरू हुई थी।
आधी रात के समय महफ़िल इतनी भीगी कि सबकी आँखें भर आईं। दिल डोले, आपी का डूब ही गया। ठाकुर उसे महफ़िल से उठा कर अंदर ले गया, शर्बत शीरा पिलाने को। फिर वहीं लिटा दिया। फिर ख़्वाजा के गीत चले तो मैं भी भीग गई। आँखें भर भर आईं। मैं हैरान, मैं तो कुछ माँग नहीं रही। मैं तो इल्तिजा नहीं कर रही। मैं तो इक ताजिर हूँ। पैसा कमाने के लिए आई हूँ। मेरी आँखें क्यों भर-भर आईं ख़्वाह-म-ख़्वाह। सो मैं बिना सोचे गाए चली गई। आँखें भर-भर आती रहीं। दिल को कुछ-कुछ होता रहा। पर मैं भीग-भीग कर गाती रही। समय बीत गया और मुझे ध्यान ही न आया कि मैं उस के समय में पाँव धर चुकी हूँ। आपी थी नहीं जो मुझे टोकती।
और फिर मुझे क्या पता था कि ख़्वाजा कौन है। मैंने तो सिर्फ़ नाम सुन रखा था। उस के गीत याद कर रखे थे। मैं तो सिर्फ़ ये जानती थी कि वो ग़रीब नवाज़ है। मैं तो ग़रीब न थी। मुझे क्या पता था कि मुझे भी नवाज़ देगा। ख़्वाह-मख़ाह, ज़बरदस्ती। मुझे क्या पता था कि उस में इतनी भी सुध-बुध नहीं कि कौन पुकार रहा है। कौन गा रहा है। कौन मँगता है। कौन ख़ाली झोली फैला रहा है। कौन भरी झोली समेट रहा है। मैं तो यही सुनती आई थी कि दुखी लोग पुकार-पुकार कर हार जाते हैं, पर कोई सुनता नहीं। मुझे क्या पता था कि इतना दयालू है, इतना नीड़े है। इतने कान खड़े रखता है।
फिर ठाकुर बोला, “सुनहरी बाई, बस इक आख़िरी फ़र्माइश, ख़्वाजा पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसी भी रंग दे रंग न छूटे। धोबिया धोए जाए सारी उमरिया।”
फिर मुझे सुध-बुध न रही। ऐसी रंग पिचकारी चली कि मैं भीग गई। और मैं ही नहीं सारी महफ़िल रंग-रंग हो गई। अंग-अंग भीगा। ख़्वाजा ने रंग घाट बना दिया। घर पहुँची तो गोया मैं, मैं न थी। दिल रोया-रोया, ध्यान खोया-खोया। किसी बात में चित्त न लगता। बैठक बेगाना दिखती, साज़ में तरब न रहा। सारंगी रोए जाती। उस्ताद नक्कू ख़ाँ बजाते पर वो रोए जाते। तबला सर पीटता, घुँघरू कहते पाँव में डाल और बन को निकल जा। वहाँ उसका झूमर नाच जो पत्ते-पत्ते, डाल-डाल से झाँक रहा है।
रोज़ दिन में तीन-चार बार ऐसी रिक़्क़त तारी होती कि भैं-भैं कर रोती। फिर हाल खेलने लगती। पीली हैरान, रूपा का मुँह खुला, आपी चुप, ये क्या हो रहा है। जब आठ दिन यही हालत रही बल्कि और बिगड़ गई तो आपी बोली, “बस पुत्तर, तेरा इस बैठक से बंधन टूट गया। दाना-पानी खत्म हो गया। तूने उस के समय में पाँव धर दिया। उस ने तुझे रंग दिया। अब तू इस धंदे जोगी नहीं रही।”
“पर कहाँ जाऊँ आपी? इस बैठक से बाहर पाँव धरने की कोई जगह भी हो मेरे लिए।”
“जिसने बुलाया है उसके दरबार में जा।” रूपा बोली।
“उस भीड़ में जाए, आपी बोली, ये लड़की जाए जिस का सुनहरी पंडा कपड़ों से बाहर झाँकता है। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। इसी कोठड़ी में रहेगी। बैठक में पाँव नहीं धरेगी।”
फिर पता नहीं क्या हुआ। रिक़्क़त ख़त्म हो गई। दिल में इक जुनून उठा कि किसी की हो जाऊँ। किसी एक की। तन-मन धन से उसी की हो जाऊँ, हो रहूँ। वो आए तो उसके जूते उतारुँ, पंखा करूँ। पाँव दाबूँ, सर में तेल की मालिश करूँ। उसके लिए पकाऊँ, मेज़ लगाऊँ, बर्तन रखूँ। उसकी बनियानें धोऊँ, कपड़े इस्त्री करूँ। आरसी का कोल बनाऊँ फिर सिरहाने खड़ी रहूँ कि कब जागे, कब पानी माँगे।
एक दिन आपी बोली, “अब क्या हाल है धिये?” मैंने रो-रो के सारी बात कह दी कि कहते हैं किसी एक की हो जा।
बोली, “वो कौन है? कोई नज़र में है क्या?”
“ऊँह! कोई नज़र में नहीं।”
“नाक नक़्शा दिखता है कभी?”
“नहीं आपी।”
“कोई बात नहीं, वो बोली, जो खूँटी पर लटकाना मक़सूद है तो आप खूँटी भेजेगा।”
दस एक दिन के बाद जब बैठक राग रंग से भरी हुई थी तो मेरी कोठड़ी का दरवाज़ा बजा। आपी दाख़िल हुई, बोली, “ख़्वाजा ने खूँटी भेज दी। अब बोल क्या कहती है?”
“कौन है?” मैंने पूछा।
“कोई ज़मींदार है। अधेड़ उम्र का है। कहता है बस एक बार बैठक में आया था। सुनहरी बाई को सुना था। जब से अब तक उसकी आवाज़ कानों में गूँजती है। दिल को बहुत समझाया। तवज्जो बटाने के बहुत जतन किए। कोई पेश नहीं गई। अब हार के तेरे दर पर आया हूँ। बोल तू क्या कहती है? मुँह माँगा दूँगा।”
मैंने कहा, “दे दे। साल के लिए बख़्श दे। जैसी तेरी मर्ज़ी।” आपी हँसने लगी। फिर बोली, “चल बैठक में उसे देख ले एक नज़र।”
“ऊँहूँ!” मैंने सर हिलाया, “नहीं आपी। उन्होंने भेजा है तो ठीक है। देखने का मतलब।”
“कितनी देर के लिए मानूँ?”
“जीवन भर के लिए।”
“सोच ले, जुआ बाश निकला तो?”
“पड़ा निकले। कैसा भी है जैसा भी निकले।”
अगले दिन बैठक में हमारा निकाह हो गया। ज़मींदार ने पैसे का ढेर लगा दिया। आपी ने रद्द कर दिया लौटा दिया। बोली, “सौदा नहीं कर रही। अपनी धी विदा कर रही हूँ, और याद रख ये ख़्वाजा की अमानत है, सँभाल कर रखियो।”
हवेली यूँ उजड़ी थी जैसे देव फिर गया हो।
वैसे तो सभी कुछ था, साज़-ओ-सामान था। आराइश थी, क़ालीन बिछे हुए थे। सोफ़े लगे हुए थे। क़द-ए-आदम आईने, झाड़ फ़ानूस सभी कुछ। फिर भी हवेली भाँय-भाँय कर रही थी। बरामदे में आराम कुर्सी पर छोटी चौधरानी बैठी हुई थी। सामने तिपाई पर चाय के बर्तन पड़े थे। मगर उसे ख़बर ही न थी कि चाय ठंडी हो चुकी है। उसे तो ख़ुद की सुध-बुध न थी कि कौन है, कहाँ है, क्यों है। ऊपर से शाम आ रही थी। समय को समय टकराती। उदासियों के झंडे गाड़ती। यादों के दिये जलाती। बीती बातों के अलाप गुनगुनाती। दबे पाँव, मद्धम। यूँ जैसे पायल की झंकार बैरनिया हो।
दूर, अपने क्वार्टर के बाहर खाट पर बैठे हुए चौकीदार की निगाहें छोटी चौधरानी पर जमी हुई थीं। हुक़्क़े का सोंटा लगाता और फिर से छोटी चौधरानी को देखने लगता। यूँ जैसे उसे देख-देख कर दुखी हुआ जा रहा हो। दूसरी जानिब घास के प्लाट के कोने पर बूढ़ा माली पौधों की तराश-ख़राश में लगा था। हर दो घड़ी के बाद सर उठाता और छोटी चौधरानी की तरफ़ टकटकी बाँध कर बैठ जाता। फिर चौंक कर लंबी ठंडी साँस भरता और फिर से काट छाँट में लग जाता।
जन्नत बीबी, जो छोटी चौधरानी का खाना पकाती थी, दो-तीन बार बरामदे के परले किनारे पर खड़ी हो कर उसे देख गई थी। जब देखती तो उस की आँखें भीग भीग जाती थीं। पल्लू से पोंछती फिर लौट जाती। अरे नौकर कमीन छोटी चौधरानी पर जान छिड़कते थे। उसके ग़म में घुले जा रहे थे। लेकिन साथ ही वो उस पर सख़्त नाराज़ भी थे। उसने अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी क्यूँ मारी थी? क्यूँ ख़ुद को दूजों का मोहताज बना लिया था? क्यूँ? अपनी औलाद होती तो फिर भी सहारा होता। अपनी औलाद भी तो थी नहीं।
जब चौधरी मरने से पहले बक़ाइमी होश-ओ-हवास अपनी आधी ग़ैर-मनक़ूला जायदाद छोटी चौधरानी के नाम गिफ्ट कर गया तो उसे क्या हक़ था कि अपना तमाम हिस्सा बड़ी चौधरानी के दोनों बेटों में तक़सीम कर दे। अगर एक दिन बड़ी चौधरानी ने उसे हवेली से निकाल बाहर किया तो वो क्या करेगी? किस का दर देखेगी?
एक तरफ़ तो इतनी बेनियाज़ी कि इतनी बड़ी जायदाद अपने हाथ से बाँट दी और दूसरी तरफ़ यूँ सोचों में गुम तस्वीर बन कर बैठ रहती है। सारे ही नौकर हैरान थे कि छोटी चौधरानी किस सोच में खोई रहती है। चौधरी को मरे हुए तीन महीने हो गए थे। जब से यूँ ही हवास गुम क़यास गुम बैठी रहती है। और फिर टूटती रात समय उस के कमरे से गुनगुनाने की आवाज़ क्यूँ आती है? किस ख़्वाजा पिया को बुलाती है? ख़्वाजा पिया मोरी लीजो खबरिया। कौन ख़बर ले? कैसी ख़बर ले? छोटी चौधरानी पर उन्हें प्यार ज़रूर आता था। पर उसकी बातें समझ में नहीं आती थीं। पता नहीं चलता था कि किस सोच में पड़ी रहती है।
छोटी चौधरानी को सिर्फ़ एक सोच थी। अंदर से एक आवाज़ उठती। बोल तेरा जीवन किस काम आया? वो सोच-सोच हार जाती, पर इस सवाल का जवाब ज़ह्न में न आता। उलझे-उलझे ख़याल उलझाते। मुझे चमन से उखेड़ा। बेल बना कर इक दरख़्त के गिर्द घुमा दिया और अब उस दरख़्त को उखेड़ फेंका। बेल मिट्टी में मिल गई। अब ये किस के गिर्द घूमे? बोल मेरा जीवन किस काम आया?
दफ़्अतन उस ने महसूस किया कि कोई उस के रू-ब-रू खड़ा है। सर उठाया, सामने गाँव का पटवारी खड़ा था।
“क्या है?” वो बोली।
“मैं हूँ पटवारी, छोटी चौधरानी जी।”
“तो जा, जा कर बड़ी चौधरानी से मिल। मुझसे तेरा क्या काम?”
“आप ही से काम है।” वो बोला।
“तो बोल क्या कहता है?”
“गाँव में दो दरवेश आए हैं। गाँव वाले चाहते हैं उन्हें चंद दिन यहाँ रोका जाए। जो आप इजाज़त दें तो आपके मेहमानख़ाने में ठहरा दें।”
“ठहरा दो।” वो बोली।
“नौकर-चाकर, बंदोबस्त…” वो रुक गया।
“सब हो जाएगा।”
पटवारी सलाम करके जाने लगा तो पता नहीं क्यों उसने सरसरी तौर पर पूछा, “कहाँ से आए हैं?”
पटवारी बोला, “अजमेर शरीफ़ से आए हैं। ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ के फ़क़ीर हैं।” इक धमाका हुआ छोटी चौधरानी की बोटियाँ हवा में उछलीं। अगली शाम छोटी चौधरानी ने जन्नत बीबी से पूछा, “जन्नत ये जो दो दरवेश ठहरे हुए हैं यहाँ, उन के पास गाँव वाले आते हैं क्या?” जन्नत बोली, “लो छोटी चौधरानी, वहाँ तो सारा दिन लोगों का ताँता लगा रहता है। बड़े पहुँचे हुए हैं, जो मुँह से कहते हैं हो जाता है।”
“तो तैयार हो जा। जन्नत हम भी जाएँगे, तू और मैं।”
“चौधरानी जी वो मग़रिब के बाद किसी से नहीं मिलते।”
“तू चल तो सही। चौधरानी ने ख़ुद को चादर में लपेटते हुए कहा, और देख, वहाँ मुझे चौधरानी कह कर न बुलाना। ख़बरदार!”
जब वो मेहमानख़ाने पहुँचीं तो दरवाज़ा बंद था। जन्नत ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? “अंदर से आवाज़ आई। जन्नत ने फिर दस्तक दी। सफेद रीश बूढ़े ख़ादिम ने दरवाज़ा खोला। जन्नत ज़बरदस्ती अंदर दाख़िल हो गई। पीछे-पीछे चौधरानी थी। सफ़ेद रीश घबरा गया। बोला, “साईं बादशाह मग़रिब के बाद किसी से नहीं मिलते। वो उस कमरे में मशग़ूल हैं।”
“हम साईं बादशाह से मिलने नहीं आए।” छोटी चौधरानी बोली।
“तो फिर?” सफ़ेद रेश घबरा गया।
“एक सवाल पूछना है।” चौधरानी ने कहा।
“साईं बाबा इस समय सवाल का जवाब नहीं देंगे।”
“साईं बाबा ने जवाब नहीं देना। उन्होंने पूछना है।” वो बोली।
“किस से पूछना है?” ख़ादिम बोला।
“उस से पूछना है जिसके वो बालिके हैं।” ये सुन कर सफ़ेद रीश ख़ादिम सन्न हो कर खड़े का खड़ा रह गया।
“उन से पूछो…” छोटी चौधरानी ने कहा, “एक औरत तेरे द्वार पर खड़ी पूछ रही है, ऐ ग़रीब नवाज़ बता कि मेरा जीवन किस काम आया?”
कमरे पर मनों बोझल ख़ामोशी तारी हो गई।
छोटी चौधरानी बोली, “कहो वो औरत पूछती है तूने बैठक के गमले से इक बूटा उखेड़ा। उसे बेल बना कर एक दरख़्त के गिर्द लपेट दिया कि जा उस पर निसार होती रह।” वो रुक गई। कमरे की ख़ामोशी और गहरी हो गई। “अब तूने उस दरख़्त को उखेड़ फेंका है। बेल मिट्टी में रुल गई। वो बेल पूछती है, बोल मेरा जीवन किस काम आया?” ये कह कर वो चुप हो गई।
“तेरा जीवन किस काम आया। तेरा जीवन किस काम आया।” सफ़ेद रीश ख़ादिम के होंट लरज़ने लगे।
“तू पूछती है तेरा जीवन किस काम आया?” वो रुक गया। कमरे की ख़ामोशी इतनी बोझल हो गई कि सहारी नहीं जाती थी।
“मेरी तरफ़ देख…” सफ़ेद रीश ख़ादिम ने कहा, “सुनहरी बाई, मेरी तरफ़ देख कि तेरा जीवन किस काम आया। मुझे नहीं पहचानती? मैं तेरा सारंगी नवाज़ था। देख मैं क्या था, क्या हो गया।”
छोटी चौधरानी से मुँह से एक चीख़ निकली, “उस्ताद जी, आप?” वो उस्ताद के चरण छूने के लिए आगे बढ़ी। ऐन उसी वक़्त मुल्हिक़ा कमरे का दरवाज़ा खुला। एक भारी भरकम नूरानी चेहरा बरामद हुआ।
“सुनहरी बीबी…” वो बोला, “मुझसे पूछ तेरा जीवन किस काम आया?”
“छोटी चौधरानी ने मुड़ कर देखा, ठाकुर! वो चिल्लाई।”
ठाकुर बोला, “अब हमें पता चला कि सरकार ने हमें इधर आने का हुक्म क्यूँ दिया था।” उसने सुनहरी बीबी के सामने अपना सर झुका दिया। बोला, “बीबी हमें आशीर्वाद दे।”
٠٠٠